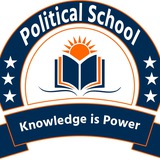Political School
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. प्राकृतिक अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं।
2. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
1. प्राकृतिक अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं।
2. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
व्याख्या-
० प्राकृतिक अधिकार (नेचुरल राईट):
✓ ये केवल एक व्यक्ति (मनुष्य) होने के आधार पर प्राप्त अधिकार हैं। प्राकृतिक कानून सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए लागू होता है, चाहे वह किसी भी आयु, लिंग, क्षेत्र आदि का हो। इसलिए कथन 1 सही है।
✓ प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन अधिकारों का राजनीतिक निहितार्थ यह है कि ये अधिकार, मनुष्य में निहित होने के कारण, राज्य की अवधारणा की शुरुआत से पहले ही मौजूद थे। इसलिए, राज्य द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
• बुनियादी अधिकार
✓ मूल अधिकारों की गारंटी देश के संविधान या कानूनी अधिनियमों द्वारा दी जाती है।
✓ इसमें 'जीवन का अधिकार' जैसे प्राकृतिक अधिकार शामिल हो सकते हैं।
✓ अलग-अलग देशों में नागरिकों को भिन्न-भिन्न मूल अधिकार प्राप्त हैं।
✓ यह आवश्यक नहीं है कि सभी मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार हों। उदाहरण के लिए, भारत में 'शिक्षा का अधिकार' मूल अधिकार है, किंतु यह प्राकृतिक अधिकार नहीं है।
इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
० प्राकृतिक अधिकार (नेचुरल राईट):
✓ ये केवल एक व्यक्ति (मनुष्य) होने के आधार पर प्राप्त अधिकार हैं। प्राकृतिक कानून सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए लागू होता है, चाहे वह किसी भी आयु, लिंग, क्षेत्र आदि का हो। इसलिए कथन 1 सही है।
✓ प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन अधिकारों का राजनीतिक निहितार्थ यह है कि ये अधिकार, मनुष्य में निहित होने के कारण, राज्य की अवधारणा की शुरुआत से पहले ही मौजूद थे। इसलिए, राज्य द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
• बुनियादी अधिकार
✓ मूल अधिकारों की गारंटी देश के संविधान या कानूनी अधिनियमों द्वारा दी जाती है।
✓ इसमें 'जीवन का अधिकार' जैसे प्राकृतिक अधिकार शामिल हो सकते हैं।
✓ अलग-अलग देशों में नागरिकों को भिन्न-भिन्न मूल अधिकार प्राप्त हैं।
✓ यह आवश्यक नहीं है कि सभी मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार हों। उदाहरण के लिए, भारत में 'शिक्षा का अधिकार' मूल अधिकार है, किंतु यह प्राकृतिक अधिकार नहीं है।
इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
👍9❤2👏2
Forwarded from Political Thoughts with Bhukar (Pramod Bhukar)
डॉ_भीमराव_अंबेडकर_और_गांधी_के_बीच_प्रमुख_मतभेद_और_विरोधाभास_.pdf
120.1 KB
👍2🔥2👏1
Forwarded from Political Thoughts with Bhukar (Pramod Bhukar)
डॉ. भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच मतभेदो का प्रश्न School Lecturer 2013, RAS-2012, School Lecturer-2022, College Lecturer-2016 में लगातार RPSC द्वारा पूछा गया है। एक बार पढ़ लें…
👍8❤2👏1
क्वाड / QUAD समिट 2024
• क्वाड (QUAD) के छठवे शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 सितम्बर को संयुक्त राज्य अमेरिका के विलमिंगटन, डेलावेयर में हुआ। इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन द्वारा की गई।
क्वाडरीलेटरल सिक्योरिटी डॉयलॉग (QUAD) चार देशों आस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के मध्य कूटनीतिक साझेदारी है।
• उद्देश्य - हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना।
• क्वाड (QUAD) की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई तथा इसकी पहली बैठक वर्ष 2007 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के दौरान हुई थी।
वर्ष 2023 में क्वाड (QUAD) की पांचवी बैठक का आयोजन हीरोशिमा (जापान) में आयोजित हुआ था |
क्वाड (QUAD) शिखर सम्मेलन घोषणाएँ
क्वाड कैंसर मूनशॉट हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से जीवन बचाने के लिए साझेदारी।
• हिंद प्रशांत के लिए नई पहल मैत्री (MAITRI) की घोषणा।
वर्ष 2025 में मुंबई (भारत) में प्रथम क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन का आयोजन।
वर्ष 2025 में समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 'क्वाड-एट- सी शिप' आब्जर्वर मिशन
• क्वाड (QUAD) देशों के मध्य सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को
मजबूत करने के लिए समझौता किया गया ।
• क्वाड स्टेम (STEM) फैलोशिप के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र के
छात्रों के लिए भारतीय सरकारी संस्थानों में 4 वर्षीय स्नातक इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान किया जायेगा।
• भारत द्वारा मॉरीशस के लिए अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना।
• बायोएक्सप्लोर पहल के अंतर्गत जैविक पारिस्थितक प्रणाली के अध्ययन में AI तकनीक के प्रयोग के लिए 2 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण |
#IR_Current_Affairs
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
• क्वाड (QUAD) के छठवे शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 सितम्बर को संयुक्त राज्य अमेरिका के विलमिंगटन, डेलावेयर में हुआ। इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन द्वारा की गई।
क्वाडरीलेटरल सिक्योरिटी डॉयलॉग (QUAD) चार देशों आस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के मध्य कूटनीतिक साझेदारी है।
• उद्देश्य - हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना।
• क्वाड (QUAD) की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई तथा इसकी पहली बैठक वर्ष 2007 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के दौरान हुई थी।
वर्ष 2023 में क्वाड (QUAD) की पांचवी बैठक का आयोजन हीरोशिमा (जापान) में आयोजित हुआ था |
क्वाड (QUAD) शिखर सम्मेलन घोषणाएँ
क्वाड कैंसर मूनशॉट हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से जीवन बचाने के लिए साझेदारी।
• हिंद प्रशांत के लिए नई पहल मैत्री (MAITRI) की घोषणा।
वर्ष 2025 में मुंबई (भारत) में प्रथम क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन का आयोजन।
वर्ष 2025 में समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 'क्वाड-एट- सी शिप' आब्जर्वर मिशन
• क्वाड (QUAD) देशों के मध्य सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को
मजबूत करने के लिए समझौता किया गया ।
• क्वाड स्टेम (STEM) फैलोशिप के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र के
छात्रों के लिए भारतीय सरकारी संस्थानों में 4 वर्षीय स्नातक इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान किया जायेगा।
• भारत द्वारा मॉरीशस के लिए अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना।
• बायोएक्सप्लोर पहल के अंतर्गत जैविक पारिस्थितक प्रणाली के अध्ययन में AI तकनीक के प्रयोग के लिए 2 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण |
#IR_Current_Affairs
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
👍10💯2
संविधान सभा ने क्रमशः केंद्रीय और राज्य विधान-मंडलों के चुनाव के लिए दो निर्वाचन आयोगों के बजाए चुनाव कराने के लिए एक ही आयोग की व्यवस्था को अपनाया। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा इस व्यवस्था को अपनाने के कारण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है?
A) यह भारत को एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघ की स्थापना के लिए संविधान सभा की योजना का हिस्सा था।
B) यह इस चिंता का कारण था कि राज्य आयोगों को राज्य कार्यपालिका द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।✅✅
C) यह उन राज्यों के व्यय को कम करने के लिए था, जो पहले से ही कल्याणकारी कार्यों के बोझ से दबे हुए थे।
D) यह दो आयोगों की उपस्थिति के कारण समन्वय और कार्य के दोहराव की चुनौतियों के कारण था।
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
A) यह भारत को एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघ की स्थापना के लिए संविधान सभा की योजना का हिस्सा था।
B) यह इस चिंता का कारण था कि राज्य आयोगों को राज्य कार्यपालिका द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।✅✅
C) यह उन राज्यों के व्यय को कम करने के लिए था, जो पहले से ही कल्याणकारी कार्यों के बोझ से दबे हुए थे।
D) यह दो आयोगों की उपस्थिति के कारण समन्वय और कार्य के दोहराव की चुनौतियों के कारण था।
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
👍9❤2👏2
Political School
संविधान सभा ने क्रमशः केंद्रीय और राज्य विधान-मंडलों के चुनाव के लिए दो निर्वाचन आयोगों के बजाए चुनाव कराने के लिए एक ही आयोग की व्यवस्था को अपनाया। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा इस व्यवस्था को अपनाने के कारण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? A) यह भारत को…
व्याख्या-
• फरवरी 1948 में संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए संविधान के प्रारूप में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को राज्य विधान-मंडलों के चुनाव का प्रभार नहीं दिया गया था। राज्य के चुनावों की जिम्मेदारी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले एक राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई थी।
• हालांकि, जब अनुच्छेद 289 का प्रारूप चर्चा के लिए आया, तो डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (प्रारूप समिति के अध्यक्ष) ने राज्य के चुनावों को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में रखते हुए एक संशोधन पेश किया।
• डॉ. अम्बेडकर ने इसके पीछे का कारण सभा को बताया कि प्रारूप समिति और केंद्र सरकार को इससे संबंधित सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के अनुसार इन प्रांतों में कार्यकारी सरकार द्वारा परिस्थितियों को इस तरह से निर्देशित या प्रबंधित किया जा रहा था कि जो लोग उनसे नस्लीय, सांस्कृतिक या भाषाई रूप से संबंधित नहीं थे उनको मतदाता सूची से बाहर रखा जा रहा था। अम्बेडकर चिंतित थे कि राज्य आयोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसलिए राज्य के चुनावों को केंद्रीय आयोग के कार्यक्षेत्र में रखना बेहतर समझा गया। इसके परिणामस्वरूप, लोक सभा और राज्य विधान-मंडलों, दोनों के लिए चुनाव कराने हेतु एकल आयोग का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया।
• इसलिए विकल्प (B) सही उत्तर है।
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
• फरवरी 1948 में संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए संविधान के प्रारूप में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को राज्य विधान-मंडलों के चुनाव का प्रभार नहीं दिया गया था। राज्य के चुनावों की जिम्मेदारी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले एक राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई थी।
• हालांकि, जब अनुच्छेद 289 का प्रारूप चर्चा के लिए आया, तो डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (प्रारूप समिति के अध्यक्ष) ने राज्य के चुनावों को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में रखते हुए एक संशोधन पेश किया।
• डॉ. अम्बेडकर ने इसके पीछे का कारण सभा को बताया कि प्रारूप समिति और केंद्र सरकार को इससे संबंधित सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के अनुसार इन प्रांतों में कार्यकारी सरकार द्वारा परिस्थितियों को इस तरह से निर्देशित या प्रबंधित किया जा रहा था कि जो लोग उनसे नस्लीय, सांस्कृतिक या भाषाई रूप से संबंधित नहीं थे उनको मतदाता सूची से बाहर रखा जा रहा था। अम्बेडकर चिंतित थे कि राज्य आयोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसलिए राज्य के चुनावों को केंद्रीय आयोग के कार्यक्षेत्र में रखना बेहतर समझा गया। इसके परिणामस्वरूप, लोक सभा और राज्य विधान-मंडलों, दोनों के लिए चुनाव कराने हेतु एकल आयोग का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया।
• इसलिए विकल्प (B) सही उत्तर है।
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
👍6❤3🔥2
राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन हेतु
किसके द्वारा संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है?
किसके द्वारा संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है?
Anonymous Quiz
36%
वासुदेव देवनानी
38%
ललित के. पँवार
20%
कालीचरण सर्राफ
6%
टीकाराम जूली
👍7❤4💯2
उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है।
2. उद्देशिका द्वारा निर्धारित उद्देश्य भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं।
3. केवल उद्देशिका का उल्लंघन करने के कारण किसी भी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
A)केवल एक
B)केवल दो
C) सभी तीन ✅✅
D) कोई नहीं
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
1. उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है।
2. उद्देशिका द्वारा निर्धारित उद्देश्य भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं।
3. केवल उद्देशिका का उल्लंघन करने के कारण किसी भी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
A)केवल एक
B)केवल दो
C) सभी तीन ✅✅
D) कोई नहीं
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
👍8👏2🙏1
Political School
उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। 2. उद्देशिका द्वारा निर्धारित उद्देश्य भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं। 3. केवल उद्देशिका का उल्लंघन करने के कारण किसी भी कानून को रद्द नहीं…
व्याख्या-
• भारत के उच्चतम न्यायालय ने मूल रूप से बेरुबाड़ी वाद (1960) में राष्ट्रपति के संदर्भ में निर्दिष्ट किया था कि उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग नहीं है और इसलिए यह न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है। हालांकि, वर्ष 1973 के केशवानंद वाद में उच्चतम न्यायालय ने पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया। साथ ही, यह माना कि उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है, जहां अलग-अलग व्याख्याएं एकमत नहीं हैं। वर्ष 1995 में केंद्र सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर निर्दिष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसलिए कथन 1 सही है।
1 • मूल रूप से अधिनियमित उद्देशिका में राज्य को "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" के रूप में वर्णित किया गया था। इसमें "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों को बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निस्सन्देह उद्देशिका, कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है। इसलिए किसी भी कानून को केवल उद्देशिका का उल्लंघन करने पर ही निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए कथन 3 सही है।
• केशवानंद मामले में उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्य, भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं। इसलिए कथन 2 सही है
इस प्रश्न का विकल्प C सही है
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
• भारत के उच्चतम न्यायालय ने मूल रूप से बेरुबाड़ी वाद (1960) में राष्ट्रपति के संदर्भ में निर्दिष्ट किया था कि उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग नहीं है और इसलिए यह न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है। हालांकि, वर्ष 1973 के केशवानंद वाद में उच्चतम न्यायालय ने पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया। साथ ही, यह माना कि उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है, जहां अलग-अलग व्याख्याएं एकमत नहीं हैं। वर्ष 1995 में केंद्र सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर निर्दिष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसलिए कथन 1 सही है।
1 • मूल रूप से अधिनियमित उद्देशिका में राज्य को "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" के रूप में वर्णित किया गया था। इसमें "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों को बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निस्सन्देह उद्देशिका, कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है। इसलिए किसी भी कानून को केवल उद्देशिका का उल्लंघन करने पर ही निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए कथन 3 सही है।
• केशवानंद मामले में उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्य, भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं। इसलिए कथन 2 सही है
इस प्रश्न का विकल्प C सही है
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
👍9❤2🙏2
Forwarded from Wader Political Science School Lecturer
किसने तर्क दिया कि हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में साधारण जन ने दंड के भय से प्रभुसत्ता कि बात मान ली?
Anonymous Quiz
14%
A. लिओ स्ट्राउस
30%
B.सी ई वॉन
43%
C. सी बी मेक्फर्सन
13%
D. सेबाईन
👍2🏆1
Forwarded from Wader Political Science School Lecturer
किसने कहा था ,” केवल वह स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है जिसमें अपने शुभ को अपनी तरह से पाने की कोशिश करने की स्वतंत्रता हो।”
Anonymous Quiz
27%
a. टी एच ग्रीन
35%
b. आईसिह बर्लिन
30%
c. जे एस मिल
8%
d. जॉन रॉल्स
👍4💯2🏆2
Forwarded from Wader Political Science School Lecturer
किसने न्याय को हर किसी को उसके हक में निरंतर और शाश्वत इच्छा के रूप में परिभाषित किया?
Anonymous Quiz
9%
अ.हॉब्स
63%
ब.जॉन रॉल्स
17%
स.प्लेटो
10%
द.जस्टिनियन
👍3❤2🔥2
Forwarded from Wader Political Science School Lecturer
लोहिया ने किस घटना के बाद कांग्रेस से अलग होकर अपनी राजनीति शुरू की?
Anonymous Quiz
11%
(a) भारत छोड़ो आंदोलन
16%
(b) द्वितीय विश्व युद्ध
56%
(c) 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद
16%
(d) गांधीजी की हत्या के बाद
👍4🔥2🎉2
Forwarded from Wader Political Science School Lecturer
“टू टाईप्स ऑफ नेशनलिज्म” के लेखक है
Anonymous Quiz
20%
A.अर्नेस्ट गेलनर
46%
B. बेनेडिक्ट एंडरसन
27%
C. जॉन प्लेननेट्ज
7%
D. हेरोल्ड लास्की
👍6🔥5⚡2🏆1
मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. विधिक अधिकारों और मूल अधिकारों, दोनों को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है।
2. मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि विधिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1, न ही 2 ✅✅
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
1. विधिक अधिकारों और मूल अधिकारों, दोनों को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है।
2. मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि विधिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1, न ही 2 ✅✅
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
👍6💯2🔥1
Political School
मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. विधिक अधिकारों और मूल अधिकारों, दोनों को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है। 2. मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि विधिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।…
व्याख्या-
० कथन 1 सही नहीं हैः मूल अधिकार, हमें उपलब्ध अन्य अधिकारों से अलग होते हैं। जहाँ, साधारण विधिक अधिकारों को साधारण विधि द्वारा संरक्षित तथा लागू किया जाता है, वहीं मूल अधिकारों को देश का संविधान संरक्षित करता है और इनकी गारंटी देता है। संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकारों के ही उपवर्ग होते हैं। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान में दिया गया है। इसे विधिक अधिकार ही कहा जाता है।
• कथन 2 भी सही नहीं हैः विधिक अधिकारों के विपरीत, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि ये संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित होते हैं। साधारण अधिकारों को विधायिका द्वारा विधि-निर्माण की साधारण प्रक्रिया से परिवर्तित किया जा सकता है, किन्तु मूल अधिकारों को केवल संविधान में संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है। इसके अलावा, सरकार का कोई संस्थान इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। हालांकि, मूल अधिकार, असीमित या पूर्ण अधिकार नहीं होते। सरकार द्वारा मूल अधिकारों की व्यावहारिकता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
इस प्रश्न का विकल्प D सही है
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
० कथन 1 सही नहीं हैः मूल अधिकार, हमें उपलब्ध अन्य अधिकारों से अलग होते हैं। जहाँ, साधारण विधिक अधिकारों को साधारण विधि द्वारा संरक्षित तथा लागू किया जाता है, वहीं मूल अधिकारों को देश का संविधान संरक्षित करता है और इनकी गारंटी देता है। संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकारों के ही उपवर्ग होते हैं। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान में दिया गया है। इसे विधिक अधिकार ही कहा जाता है।
• कथन 2 भी सही नहीं हैः विधिक अधिकारों के विपरीत, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि ये संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित होते हैं। साधारण अधिकारों को विधायिका द्वारा विधि-निर्माण की साधारण प्रक्रिया से परिवर्तित किया जा सकता है, किन्तु मूल अधिकारों को केवल संविधान में संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है। इसके अलावा, सरकार का कोई संस्थान इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। हालांकि, मूल अधिकार, असीमित या पूर्ण अधिकार नहीं होते। सरकार द्वारा मूल अधिकारों की व्यावहारिकता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
इस प्रश्न का विकल्प D सही है
https://t.me/pol_sci_with_devrajgaur
👍8🔥2💯1