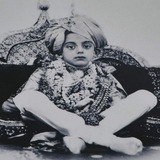"इस देश में ' आम ' नामक एक फल होता है , जिसका वृक्ष होता तो नारंगी की भांति है ...परन्तु डील - डौल में उससे कहीं अधिक बड़ा होता है और पत्ते खूब सघन होते हैं । इस वृक्ष की छाया खूब होती है परन्तु इसके नीचे सोने से लोग आलसी हो जाते हैं । फल अर्थात् आम ' आलू बुख़ारे ' से बड़ा होता है । पकने से पहले यह फल देखने में हरा दीखता है । जिस प्रकार हमारे देश ( मोरक्को ) में नींबू तथा खट्टे का अचार बनाया जाता है , उसी प्रकार कच्ची दशा में पेड़ से गिरने पर इस फल का भी नमक डालकर लोग अचार बनाते हैं । आम के अतिरिक्त इस देश में अदरक और मिर्च का भी अचार बनाया जाता है । अचार को लोग भोजन के साथ खाते हैं , प्रत्येक ग्रास के पश्चात् थोड़ा सा अचार खाने की प्रथा है । ख़रीफ़ में आम पकने पर पीले रंग का हो जाता है ...और सेव की भांति खाया जाता है । कोई चाकू से छीलकर खाता है ...तो कोई यों ही चूस लेता है । आम की मिठास में कुछ खट्टापन भी होता है । इस फल की गुठली भी बड़ी होती है ....जिसे बो देने पर वृक्ष लग जाता है ।"
--इब्नबतूता का भारत वर्णन
-----&-----
आश्चर्य है एक विदेशी...भारत की हर वस्तु का इतना उत्तम विवरण...छोड़ गया है..यानि एक फल को लें...तो उसकी गुठली से लेकर वृक्ष..कच्चे प्रयोग ...पक्के प्रयोग...विविध उपयोग..दुरुपयोग..का विवरण।
--इब्नबतूता का भारत वर्णन
-----&-----
आश्चर्य है एक विदेशी...भारत की हर वस्तु का इतना उत्तम विवरण...छोड़ गया है..यानि एक फल को लें...तो उसकी गुठली से लेकर वृक्ष..कच्चे प्रयोग ...पक्के प्रयोग...विविध उपयोग..दुरुपयोग..का विवरण।
दक्षिण भारत में नागर शैली मन्दिर
----------------------------------------
दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के आरंभ के उदाहरण मैसूर के बीजापुर जिले के अंतर्गत ऐहोल के पाषाणनिर्मित मंदिर में मिलते हैं । यदि गंभीरतापूर्वक देखा जाये तो.. उत्तरी भारत के ' नागर शैली ' का विस्तार कृष्णा - तुंगभ्रदा घाटी में भी हुआ । नागर शैली के इस विस्तार के भी दो उपविभाग किए जा सकते हैं । सबसे प्रथम विस्तार कृष्णा - तुंगभद्रा घाटी में हुआ जहाँ द्रविड़ शैली के साथ ऐहोल के मंदिर , पट्टड़कल तथा आलमपुर की स्थापत्यकला नागर रीति के साथ संपन्न हुई है । यहीं दोनों शैलियों ( नागर तथा द्राविड़ ) का संगम मिलता है । खानदेश के समीपवर्ती भू - भाग में भी नागर शैली की इमारतें वर्तमान हैं ।
दोनों शैलियों की विशेषताएँ तथा तत्त्वों के सम्मिश्रण से चालुक्य शैली का जन्म हुआ ... यही आगे चल कर एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शैली के रूप में सामने आता है ।
बीजापुर जिले का ऐहोल नामक स्थान... इमारतों का संग्रहालय है , जिसमें कुछ उसके प्राचीन गौरव को बतलाती हैं । इन मंदिरों का निर्माण 450 ई ० से 600 ई ० के मध्य चालुक्य राजाओं ने कराया था । संभवत : आर्यन शिखर ( नागर शैली ) का प्रभाव दक्षिण पहुँचा ... इस कारण ऐहोल के मंदिरों में मिश्रित शैली मिलती है । इस स्थान के 70 मंदिरों में नागर स्थापत्य के विचार अनेक इमारतों में प्रकट होते हैं ।
ऐहोल के मंदिर को चालुक्य स्थापत्यकला का जन्मदाता कह सकते हैं । ऐहोल के मंदिर के गर्भगृह त्रिरत्ल योजना पर बने हैं .... उस पर छोटा शिखर है और मंदिर के सामने के भाग में स्तंभयुक्त कमरा है ।
नागर शैली के प्रारंभिक शिखर की रूपरेखा ऐहोल के मंदिरों में वर्तमान है ।
ऐहोल में स्थापत्य कार्य का उत्साहवर्द्धक आरंभ दो सदियों तक चलता रहा । बादामी से 16 किलोमीटर दूर पट्टड़कल में आज भी मंदिरों का जमघट है । इसमें कई मंदिर उत्तरी यानी नागर वास्तु शैली के हैं , जो पाँचवीं सदी में बने थे ---
पापनाथ मन्दिर
जम्बूलिंग मन्दिर
करसिद्धेश्वर मन्दिर
काशी विश्वनाथ मन्दिर।
-- सातवीं सदी में निर्मित नागर शैली के पापनाथ मंदिर.. स्थापत्य कला में अन्य मंदिरों से उत्तम तथा प्रभावोत्पादक है । पापनाथ का मंदिर विशाल ठोस चट्टानों से निर्मित है । दीवारों एवं स्तंभ विशालकाय दीख पड़ते हैं ।
काशी विश्वनाथ के ... मंदिर में गर्भगृह त्रिरत्न योजना सहित बनाया गया , जिसके ऊपरी भाग में शिखर विद्यमान हैं । यह सभी ऐहोल तथा उत्तरी भारत के स्थापत्य मंदिरों के नमूनों के समान है । दक्षिण भारत की आरंभिक शिखर शैली में आमलक भी दीख पड़ते हैं । पट्टड़कल के पापनाथ मंदिर में ढका प्रदक्षिणा मार्ग है , जिससे संबद्ध दो प्रकोष्ठ हैं । एक को अंतराल तथा दूसरे को सभामंडप कहा जा सकता है । गर्भगृह की छत चिपटी है , जिसके ऊपर शिखर स्थित है । अन्य बनावट तथा तत्त्वों को ध्यान में रखकर यह कहना यथार्थ होगा कि नागर शैली की मीनार को छोड़ कर समस्त आकार द्रविड़ रीति के विरुपाक्ष मंदिर के सदृश है ।
तुंगभद्रा के पश्चिमी किनारे पर आलमपुर में छह मंदिरों का समूह है , जो पापनाथ से मिलता - जुलता है । दक्षिण भारत में नागर वास्तुकला के विस्तार में शिखर की प्रधानता है , जो स्थानीय अन्य आकार - प्रकार से उसे पृथक् करता है । इसमें मुख्य मीनार के साथ अंगशिखर की आवश्यकता का अनुभव उस रूप से नहीं किया गया । परंतु , उड़ीसा तथा दक्षिण की नागर शैली में मुख्य शिखर से अंगशिखर को गौण स्थान दिया गया है । इस कारण कालांतर में अंग शिखर अप्रधान हो गए और स्वतंत्रता खो बैठे । स्टेला क्रेमरीश इस आकार को संग्रथित रूप मानती हैं , जिसमें दोनों को ( मुख्यतया अंगशिखर ) मिश्रित करने का सफल प्रयत्न किया गया ।
-------------
Pappusingh prajapat
Pic- पापनाथ मन्दिर
----------------------------------------
दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के आरंभ के उदाहरण मैसूर के बीजापुर जिले के अंतर्गत ऐहोल के पाषाणनिर्मित मंदिर में मिलते हैं । यदि गंभीरतापूर्वक देखा जाये तो.. उत्तरी भारत के ' नागर शैली ' का विस्तार कृष्णा - तुंगभ्रदा घाटी में भी हुआ । नागर शैली के इस विस्तार के भी दो उपविभाग किए जा सकते हैं । सबसे प्रथम विस्तार कृष्णा - तुंगभद्रा घाटी में हुआ जहाँ द्रविड़ शैली के साथ ऐहोल के मंदिर , पट्टड़कल तथा आलमपुर की स्थापत्यकला नागर रीति के साथ संपन्न हुई है । यहीं दोनों शैलियों ( नागर तथा द्राविड़ ) का संगम मिलता है । खानदेश के समीपवर्ती भू - भाग में भी नागर शैली की इमारतें वर्तमान हैं ।
दोनों शैलियों की विशेषताएँ तथा तत्त्वों के सम्मिश्रण से चालुक्य शैली का जन्म हुआ ... यही आगे चल कर एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शैली के रूप में सामने आता है ।
बीजापुर जिले का ऐहोल नामक स्थान... इमारतों का संग्रहालय है , जिसमें कुछ उसके प्राचीन गौरव को बतलाती हैं । इन मंदिरों का निर्माण 450 ई ० से 600 ई ० के मध्य चालुक्य राजाओं ने कराया था । संभवत : आर्यन शिखर ( नागर शैली ) का प्रभाव दक्षिण पहुँचा ... इस कारण ऐहोल के मंदिरों में मिश्रित शैली मिलती है । इस स्थान के 70 मंदिरों में नागर स्थापत्य के विचार अनेक इमारतों में प्रकट होते हैं ।
ऐहोल के मंदिर को चालुक्य स्थापत्यकला का जन्मदाता कह सकते हैं । ऐहोल के मंदिर के गर्भगृह त्रिरत्ल योजना पर बने हैं .... उस पर छोटा शिखर है और मंदिर के सामने के भाग में स्तंभयुक्त कमरा है ।
नागर शैली के प्रारंभिक शिखर की रूपरेखा ऐहोल के मंदिरों में वर्तमान है ।
ऐहोल में स्थापत्य कार्य का उत्साहवर्द्धक आरंभ दो सदियों तक चलता रहा । बादामी से 16 किलोमीटर दूर पट्टड़कल में आज भी मंदिरों का जमघट है । इसमें कई मंदिर उत्तरी यानी नागर वास्तु शैली के हैं , जो पाँचवीं सदी में बने थे ---
पापनाथ मन्दिर
जम्बूलिंग मन्दिर
करसिद्धेश्वर मन्दिर
काशी विश्वनाथ मन्दिर।
-- सातवीं सदी में निर्मित नागर शैली के पापनाथ मंदिर.. स्थापत्य कला में अन्य मंदिरों से उत्तम तथा प्रभावोत्पादक है । पापनाथ का मंदिर विशाल ठोस चट्टानों से निर्मित है । दीवारों एवं स्तंभ विशालकाय दीख पड़ते हैं ।
काशी विश्वनाथ के ... मंदिर में गर्भगृह त्रिरत्न योजना सहित बनाया गया , जिसके ऊपरी भाग में शिखर विद्यमान हैं । यह सभी ऐहोल तथा उत्तरी भारत के स्थापत्य मंदिरों के नमूनों के समान है । दक्षिण भारत की आरंभिक शिखर शैली में आमलक भी दीख पड़ते हैं । पट्टड़कल के पापनाथ मंदिर में ढका प्रदक्षिणा मार्ग है , जिससे संबद्ध दो प्रकोष्ठ हैं । एक को अंतराल तथा दूसरे को सभामंडप कहा जा सकता है । गर्भगृह की छत चिपटी है , जिसके ऊपर शिखर स्थित है । अन्य बनावट तथा तत्त्वों को ध्यान में रखकर यह कहना यथार्थ होगा कि नागर शैली की मीनार को छोड़ कर समस्त आकार द्रविड़ रीति के विरुपाक्ष मंदिर के सदृश है ।
तुंगभद्रा के पश्चिमी किनारे पर आलमपुर में छह मंदिरों का समूह है , जो पापनाथ से मिलता - जुलता है । दक्षिण भारत में नागर वास्तुकला के विस्तार में शिखर की प्रधानता है , जो स्थानीय अन्य आकार - प्रकार से उसे पृथक् करता है । इसमें मुख्य मीनार के साथ अंगशिखर की आवश्यकता का अनुभव उस रूप से नहीं किया गया । परंतु , उड़ीसा तथा दक्षिण की नागर शैली में मुख्य शिखर से अंगशिखर को गौण स्थान दिया गया है । इस कारण कालांतर में अंग शिखर अप्रधान हो गए और स्वतंत्रता खो बैठे । स्टेला क्रेमरीश इस आकार को संग्रथित रूप मानती हैं , जिसमें दोनों को ( मुख्यतया अंगशिखर ) मिश्रित करने का सफल प्रयत्न किया गया ।
-------------
Pappusingh prajapat
Pic- पापनाथ मन्दिर
"भगवान सूर्य" की सजीव प्रतिमा....!
शिल्पी ने प्रतिमा का निर्माण पुरा मन लगाकर किया है जिससे प्रतिमा ऐसी जीवन्त बन गयी है कि लगता है भगवान सूर्य अभी अपने नेत्र खोलकर पुरे संसार मे ऐसी रोशनी बिखेर देगे जिससे हर प्राणी मात्र तृप्त हो जायेगा. एक ग्राम मे अपेक्षित इस सजीव प्रतिमा के मुख मण्डल मे ऐसा आकर्षण बस्तर के किसी प्रतिमा मे देखने को नहीं मिला.
यह जीवित सी लगने वाली प्रतिमा भगवान सूर्य की है. प्रतिमा मे दोनो हाथ खंडित है किन्तु कन्धे पर कमल की कलियों के अंकन से प्रतीत होता है कि दोनों हाथो मे सनाल कमल कलियाँ धारित रही होगी.
चरणो मे भगवान सूर्य की अन्य प्रतिमाओ की तरह लम्बे बूट का अभाव है. हालाकि नाग शासन काल मे निर्मित यह प्रतिमा प्रकृति और उपेक्षा की मार से क्षरित हो गयी है तथापि इसके मुख मण्डल का अप्रतिम सौन्दर्य अभी भी काफ़ी प्रभाव शाली है.
सिर पर मुकुट धारण किये और कानो मे बड़े बड़े कुण्डल पहने हुए सूर्य देव की प्रतिमा रौद्र एवं सौम्यता का मिश्रित भाव लिये हुए है. एक तरफ़ अधिक क्षरित होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान सूर्य क्रोधित है एवम वही दुसरी तरफ़ से सौम्यता का भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है.
उस शिल्पकार को नमन जिसने इस जीवन्त प्रतिमा का निर्माण किया.
ओम्
आप हमे instagram मे @bastar_bhushan follow कर सकते हैं...!
शिल्पी ने प्रतिमा का निर्माण पुरा मन लगाकर किया है जिससे प्रतिमा ऐसी जीवन्त बन गयी है कि लगता है भगवान सूर्य अभी अपने नेत्र खोलकर पुरे संसार मे ऐसी रोशनी बिखेर देगे जिससे हर प्राणी मात्र तृप्त हो जायेगा. एक ग्राम मे अपेक्षित इस सजीव प्रतिमा के मुख मण्डल मे ऐसा आकर्षण बस्तर के किसी प्रतिमा मे देखने को नहीं मिला.
यह जीवित सी लगने वाली प्रतिमा भगवान सूर्य की है. प्रतिमा मे दोनो हाथ खंडित है किन्तु कन्धे पर कमल की कलियों के अंकन से प्रतीत होता है कि दोनों हाथो मे सनाल कमल कलियाँ धारित रही होगी.
चरणो मे भगवान सूर्य की अन्य प्रतिमाओ की तरह लम्बे बूट का अभाव है. हालाकि नाग शासन काल मे निर्मित यह प्रतिमा प्रकृति और उपेक्षा की मार से क्षरित हो गयी है तथापि इसके मुख मण्डल का अप्रतिम सौन्दर्य अभी भी काफ़ी प्रभाव शाली है.
सिर पर मुकुट धारण किये और कानो मे बड़े बड़े कुण्डल पहने हुए सूर्य देव की प्रतिमा रौद्र एवं सौम्यता का मिश्रित भाव लिये हुए है. एक तरफ़ अधिक क्षरित होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान सूर्य क्रोधित है एवम वही दुसरी तरफ़ से सौम्यता का भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है.
उस शिल्पकार को नमन जिसने इस जीवन्त प्रतिमा का निर्माण किया.
ओम्
आप हमे instagram मे @bastar_bhushan follow कर सकते हैं...!
पान 💚पत्ता-सुपारी
---------------------
अरब वृत्तान्तकार अबू जईद ने लिखा है कि-- मेहमानों को पान पेश करना सम्मान और मित्रता का द्योतक था ।
राजराज चोल के एक अभिलेख में तांबूल के आदान - प्रदान की पुरानी प्रथा का उल्लेख हुआ है ।
चीनी यात्री चाऊ - जू - कुआ ने राजाओं और सरदारों के बीच पान की लोकप्रियता का जिक्र किया है ।
अमीर खुसरो ने--- पान के 42 स्पष्ट गुणों का विस्तृत विवरण दिया है.... हिन्दुस्तानी इसे नाग - बेल भी कहते थे... बनारस के पान अत्यन्त लोकप्रिय थे ।
अलबेरुनी--- हिन्दुओं के पान खाने के अभ्यास का उल्लेख करते हुए कहता है , ‘ सुपारी को पान एवं चूने में मिलाकर खाने के परिणामस्वरूप उनके दाँत लाल होते है...तथा साथ में सुपारी चबाने से मसूढे व उदर मजबूत रहते हैं।
भारतीय किस प्रकार पान का प्रयोग करते हैं ...इसके सम्बन्ध में अब्दुर्रज्जाक कहता है — ' इसे खाने की निम्न विधि है : वे लोग फाउफेल ( सुपारी ) को जिसे ' सिपारी ' भी कहते हैं , कुचल कर मुँह में रखते हैं ... एक बार में पान की चार पत्तियाँ भी खा लेते हैं और चबाते हैं । कभी - कभी वे इसमें कर्पूर मिश्रित कर लेते हैं और कभी - कभी इसकी पीक थूक देते हैं जिसका रंग लाल होता है।' वह आगे लिखता है , ' इसका सार मुखड़े को एक उज्जवलता प्रदान करता है , मदिरा की भाँति उन्माद ( नशा ) उत्पन्न करता है , भूख को शान्त करता तथा आनन्द संवेग देता है । '
इब्नबतूता भी पान का उत्तम विवरण देता है---
"पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर - लता की तरह ही उगाया जाता है ; ... पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है ... इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है ; यह जायफल जैसी ही होती है पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे - छोटे टुकड़े नहीं हो जाते ; और इन्हें मुँह में रख कर चबाया जाता है । इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है ।"
----
Pappusingh prajapat
---------------------
अरब वृत्तान्तकार अबू जईद ने लिखा है कि-- मेहमानों को पान पेश करना सम्मान और मित्रता का द्योतक था ।
राजराज चोल के एक अभिलेख में तांबूल के आदान - प्रदान की पुरानी प्रथा का उल्लेख हुआ है ।
चीनी यात्री चाऊ - जू - कुआ ने राजाओं और सरदारों के बीच पान की लोकप्रियता का जिक्र किया है ।
अमीर खुसरो ने--- पान के 42 स्पष्ट गुणों का विस्तृत विवरण दिया है.... हिन्दुस्तानी इसे नाग - बेल भी कहते थे... बनारस के पान अत्यन्त लोकप्रिय थे ।
अलबेरुनी--- हिन्दुओं के पान खाने के अभ्यास का उल्लेख करते हुए कहता है , ‘ सुपारी को पान एवं चूने में मिलाकर खाने के परिणामस्वरूप उनके दाँत लाल होते है...तथा साथ में सुपारी चबाने से मसूढे व उदर मजबूत रहते हैं।
भारतीय किस प्रकार पान का प्रयोग करते हैं ...इसके सम्बन्ध में अब्दुर्रज्जाक कहता है — ' इसे खाने की निम्न विधि है : वे लोग फाउफेल ( सुपारी ) को जिसे ' सिपारी ' भी कहते हैं , कुचल कर मुँह में रखते हैं ... एक बार में पान की चार पत्तियाँ भी खा लेते हैं और चबाते हैं । कभी - कभी वे इसमें कर्पूर मिश्रित कर लेते हैं और कभी - कभी इसकी पीक थूक देते हैं जिसका रंग लाल होता है।' वह आगे लिखता है , ' इसका सार मुखड़े को एक उज्जवलता प्रदान करता है , मदिरा की भाँति उन्माद ( नशा ) उत्पन्न करता है , भूख को शान्त करता तथा आनन्द संवेग देता है । '
इब्नबतूता भी पान का उत्तम विवरण देता है---
"पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर - लता की तरह ही उगाया जाता है ; ... पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है ... इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है ; यह जायफल जैसी ही होती है पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे - छोटे टुकड़े नहीं हो जाते ; और इन्हें मुँह में रख कर चबाया जाता है । इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है ।"
----
Pappusingh prajapat
मित्रता के प्रतीक - कुड़ई फूल.....!
बस्तर के जंगल इन दिनों कुड़ई फूल यानि कुटज की महक से गमक उठे हैं, ऐसा लगता है मानों कुदरत ने आगंतुकों के स्वागत में अगरबत्ती सुलगा रखी हो।
बन्द गाड़ियों में बैठकर इसे महसूस नहीं किया जा सकता।
वैसे आयुर्वेद में भी कुटज का खास इस्तेमाल किया जाता है। अतिसार, संग्रहणी जैसे पेट के रोगों में इसकी दवा को कारगर माना जाता है। कुटज घन वटी, कुटजारिष्ट इससे ही तैयार की जाती है।
और हां, बस्तर में पुराने समय में मित्रता कायम करने के लिए कुड़ई फूल का भी आश्रय लिया जाता था। इसे मीत बदना कहा जाता था। जिसे कुड़ई फूल बद लिया यानि मान लिया तो फिर दोनों आजीवन एक दूसरे को वास्तविक नाम से नहीं, बल्कि कुड़ई फूल कहकर संबोधित किया करते थे। ठीक उसी तरह, जैसे यहां कोदोमाली, डांडामाली, भोजली(जवारा) बदने की प्रथा प्रचलित थी।
खैर, समय के साथ न तो ये उपमेय बाकी रहे, न ही उपमान। आधुनिकता की चकाचौंध ने ग्राम्य जीवन शैली को कोरोना की तरह संक्रमित जो कर दिया है।
शहरीकरण की अंधी दौड़ में न तो कुड़ई फूल, कोदोमाली जैसे वनस्पति बाकी रह गए, बल्कि और भी ऐसे प्रतिमान लुप्त होते जा रहे हैं।
साभार -शैलेन्द्र ठाकुर, दंतेवाड़ा
बस्तर के जंगल इन दिनों कुड़ई फूल यानि कुटज की महक से गमक उठे हैं, ऐसा लगता है मानों कुदरत ने आगंतुकों के स्वागत में अगरबत्ती सुलगा रखी हो।
बन्द गाड़ियों में बैठकर इसे महसूस नहीं किया जा सकता।
वैसे आयुर्वेद में भी कुटज का खास इस्तेमाल किया जाता है। अतिसार, संग्रहणी जैसे पेट के रोगों में इसकी दवा को कारगर माना जाता है। कुटज घन वटी, कुटजारिष्ट इससे ही तैयार की जाती है।
और हां, बस्तर में पुराने समय में मित्रता कायम करने के लिए कुड़ई फूल का भी आश्रय लिया जाता था। इसे मीत बदना कहा जाता था। जिसे कुड़ई फूल बद लिया यानि मान लिया तो फिर दोनों आजीवन एक दूसरे को वास्तविक नाम से नहीं, बल्कि कुड़ई फूल कहकर संबोधित किया करते थे। ठीक उसी तरह, जैसे यहां कोदोमाली, डांडामाली, भोजली(जवारा) बदने की प्रथा प्रचलित थी।
खैर, समय के साथ न तो ये उपमेय बाकी रहे, न ही उपमान। आधुनिकता की चकाचौंध ने ग्राम्य जीवन शैली को कोरोना की तरह संक्रमित जो कर दिया है।
शहरीकरण की अंधी दौड़ में न तो कुड़ई फूल, कोदोमाली जैसे वनस्पति बाकी रह गए, बल्कि और भी ऐसे प्रतिमान लुप्त होते जा रहे हैं।
साभार -शैलेन्द्र ठाकुर, दंतेवाड़ा
पंचतन्त्र के अनुवाद -
----------------------------------------------------
विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनूदित होने वाली कृतियों में से एक है --पंचतन्त्र।
570 ईस्वी में, फारस के सस्सानिद शासक खुसरो प्रथम के दरबार में रहने वाले बुर्जॉय /बुर्जोआ नामक एक ईरानी चिकित्सक ने ज्ञान की एक पुस्तक की तलाश में भारत की यात्रा की...यानि एक ऐसी किताब जो खुसरो को अमतत्व दिलाती।
सम्भवत: वह ऐसी पुस्तक की खोज में सफल रहा।
वापस लौटकर उसने तात्कालीन वज़ीर वज़ुर्गमिहर से "पंचतन्त्र "नामक इस कृति का पहलवी में " कारीक उद दमनक" नाम से अनुवाद करवाया ।यह पंचतन्त्र का प्रथम विदेशी अनुवाद था।
यह बुर्ज़ॉय की किताब ही थी-- जो दो शताब्दियों बाद (750 ई.) में हुए अरबी अनुवाद --- "कलीला वा दिमनाह" का आधार बना।
सोलहवीं शताब्दी (1504) की शुरुआत में, हेरात के तैमूरी शासक हुसैन मिर्जा बयाकार के दरबार में ...हुसैन बिन 'अली अल वाज़ काशेफ़ी ने पंचतन्त्र का फारसी अनुवाद "अनवर इ सुहिली" (lights of canopis) के नाम से लिखा ।
.. यह वह संस्करण था जिसने अबुल फ़ज़ल द्वारा पंचतन्त्र के फारसी अनुवाद " आयर-ए-दानिश" (touchstone of intellect) के लिए आधार के रूप में कार्य किया था।
पंचतंत्र का एक और संस्करण था जिसका अनुवाद अकबर के दरबार में मुस्तफा खलीकाद अब्बासी द्वारा किया गया था --वह नौंवी शताब्दी के जैन मूल के एक संस्कृत संस्करण पर आधारित था।
. अनुवाद विभाग को "मकतबखाना" कहा जाता था।
फारसी अनुवाद --अनवर इ सुहेली का उपयोग कुछ समय के लिए एक पाठ्यपुस्तक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज -हैलेबरी में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था. आयर-ए-दानिश का 1803 में मौलवी हफीजुद्दीन अहमद द्वारा उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया था।
-------------
Pappusingh prajapat
----------------------------------------------------
विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनूदित होने वाली कृतियों में से एक है --पंचतन्त्र।
570 ईस्वी में, फारस के सस्सानिद शासक खुसरो प्रथम के दरबार में रहने वाले बुर्जॉय /बुर्जोआ नामक एक ईरानी चिकित्सक ने ज्ञान की एक पुस्तक की तलाश में भारत की यात्रा की...यानि एक ऐसी किताब जो खुसरो को अमतत्व दिलाती।
सम्भवत: वह ऐसी पुस्तक की खोज में सफल रहा।
वापस लौटकर उसने तात्कालीन वज़ीर वज़ुर्गमिहर से "पंचतन्त्र "नामक इस कृति का पहलवी में " कारीक उद दमनक" नाम से अनुवाद करवाया ।यह पंचतन्त्र का प्रथम विदेशी अनुवाद था।
यह बुर्ज़ॉय की किताब ही थी-- जो दो शताब्दियों बाद (750 ई.) में हुए अरबी अनुवाद --- "कलीला वा दिमनाह" का आधार बना।
सोलहवीं शताब्दी (1504) की शुरुआत में, हेरात के तैमूरी शासक हुसैन मिर्जा बयाकार के दरबार में ...हुसैन बिन 'अली अल वाज़ काशेफ़ी ने पंचतन्त्र का फारसी अनुवाद "अनवर इ सुहिली" (lights of canopis) के नाम से लिखा ।
.. यह वह संस्करण था जिसने अबुल फ़ज़ल द्वारा पंचतन्त्र के फारसी अनुवाद " आयर-ए-दानिश" (touchstone of intellect) के लिए आधार के रूप में कार्य किया था।
पंचतंत्र का एक और संस्करण था जिसका अनुवाद अकबर के दरबार में मुस्तफा खलीकाद अब्बासी द्वारा किया गया था --वह नौंवी शताब्दी के जैन मूल के एक संस्कृत संस्करण पर आधारित था।
. अनुवाद विभाग को "मकतबखाना" कहा जाता था।
फारसी अनुवाद --अनवर इ सुहेली का उपयोग कुछ समय के लिए एक पाठ्यपुस्तक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज -हैलेबरी में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था. आयर-ए-दानिश का 1803 में मौलवी हफीजुद्दीन अहमद द्वारा उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया था।
-------------
Pappusingh prajapat
राष्ट्रवादी इतिहासकार ----यदुनाथ सरकार
----- ---
10 दिसम्बर 1870-19 मई 1958
---------------------------------------------
भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का जन्म राजशाही ( बांग्लादेश ) के करछमरिया नामक गांव में .. कायस्थ परिवार में हुआ था ।
वे सन् 1917 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर रहे , किन्तु अगले वर्ष ही रेवेशा कॉलेज , उत्कल चले गये । सन् 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारतीय शिक्षा सेवा में नियुक्त किया । अवकाश ग्रहण करने के बाद दो वर्ष के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के अवैतनिक उपकुलपति रहे ।
... सन् 1929 ब्रिटिश सरकार ने उन्हें “ सर ' की उपाधि प्रदान की ।
यदुनाथ सरकार की पहली पुस्तक ' इंडिया ऑफ औरंगजेब , टोपोग्राफी , स्टेटिस्टिक्स एण्ड रोड्स ' सन् 1901 ई . में प्रकाशित हुई तथा इसी क्रम में सन् 1919 ई . में दो खण्डों में प्रकाशित पुस्तक "हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब" इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है ...इस पुस्तक का पांचवा तथा अंतिम खण्ड सन् 1928 ई . में छपा ।
इनका शोध ग्रंथ 'शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स ' भी सन् 1919 ई . में प्रकाशित हुआ जिसमें फारसी , मराठी , राजस्थानी और यूरोपीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्री का सावधानी से उपयोग कर यदुनाथ सरकार ने ऐतिहासिक खोज का महत्वपूर्ण कार्य किया और मूलभूत स्रोतों के आधार पर शोध करने की परंपरा को दृढ़ किया । विशेष रूप से जयपुर राज्य में सुरक्षित फारसी अखबार और अन्य अभिलेखों की ओर इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित करने और उनको शोध कार्य के लिए उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य यदुनाथ सरकार ने किया ।
यदुनाथ सरकार ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विशेष रूप से औरंगजेब कालीन शोध प्रकाशित किये ।
4 भागों में -- "मुगल साम्राज्य का पतन "," मुगलशासन" ( 1925 ) ' एवं ' ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब ",बिहार एण्ड उड़ीसा ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ' सन् 1932 ई . में प्रकाशित हुई एवं सन् 1940 ई . में" हाउस ऑफ शिवाजी" की रचना की गई जिसमें यदुनाथ सरकार ने शिवाजी एवं मराठा शक्ति का वर्णन किया है ।
इनकी... "मिलिटरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया" सन् 1960 ई . में प्रकाशित हुई ।
"हिस्ट्री ऑफ बंगाल", "इण्डिया आफ्टर इण्डिपेन्डेन्स" --भी इनकी अन्य रचनाएं हैं।
इसके साथ - साथ जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह ( द्वितीय ) के आग्रह पर इन्होंने जयपुर राज्य का इतिहास" द हिस्ट्री ऑफ जयपुर "की रचना की ।
आधुनिक काल के इतिहासकारों में विशेषकर उत्तर मध्यकालीन भारत का यदुनाथ सरकार ने जितना अच्छा अध्ययन करके प्रस्तुत किया उतना उनके बाद देखने को नहीं मिला..।
.अद्यतन इनकी पुण्यतिथि होने के साथ ही...इस वर्ष 150वीं जयन्ती भी है..इस अवसर पर ..... इतिहास का विद्यार्थी..उनको ..उनके कार्यों को स्मरण कर..स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है।
...इनका इतिहास लेखन मौलिक स्रोतों पर ही आधारित रहा है तथा इन पर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने प्रशस्ति में लिखा है-- कि वे भारत के महान इतिहासकार थे और उन्होंने मध्यकालीन भारत पर निष्ठापूर्वक कार्य किया है ।
--------
Pappusingh prajapat
----- ---
10 दिसम्बर 1870-19 मई 1958
---------------------------------------------
भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का जन्म राजशाही ( बांग्लादेश ) के करछमरिया नामक गांव में .. कायस्थ परिवार में हुआ था ।
वे सन् 1917 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर रहे , किन्तु अगले वर्ष ही रेवेशा कॉलेज , उत्कल चले गये । सन् 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारतीय शिक्षा सेवा में नियुक्त किया । अवकाश ग्रहण करने के बाद दो वर्ष के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के अवैतनिक उपकुलपति रहे ।
... सन् 1929 ब्रिटिश सरकार ने उन्हें “ सर ' की उपाधि प्रदान की ।
यदुनाथ सरकार की पहली पुस्तक ' इंडिया ऑफ औरंगजेब , टोपोग्राफी , स्टेटिस्टिक्स एण्ड रोड्स ' सन् 1901 ई . में प्रकाशित हुई तथा इसी क्रम में सन् 1919 ई . में दो खण्डों में प्रकाशित पुस्तक "हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब" इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है ...इस पुस्तक का पांचवा तथा अंतिम खण्ड सन् 1928 ई . में छपा ।
इनका शोध ग्रंथ 'शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स ' भी सन् 1919 ई . में प्रकाशित हुआ जिसमें फारसी , मराठी , राजस्थानी और यूरोपीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्री का सावधानी से उपयोग कर यदुनाथ सरकार ने ऐतिहासिक खोज का महत्वपूर्ण कार्य किया और मूलभूत स्रोतों के आधार पर शोध करने की परंपरा को दृढ़ किया । विशेष रूप से जयपुर राज्य में सुरक्षित फारसी अखबार और अन्य अभिलेखों की ओर इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित करने और उनको शोध कार्य के लिए उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य यदुनाथ सरकार ने किया ।
यदुनाथ सरकार ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विशेष रूप से औरंगजेब कालीन शोध प्रकाशित किये ।
4 भागों में -- "मुगल साम्राज्य का पतन "," मुगलशासन" ( 1925 ) ' एवं ' ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब ",बिहार एण्ड उड़ीसा ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ' सन् 1932 ई . में प्रकाशित हुई एवं सन् 1940 ई . में" हाउस ऑफ शिवाजी" की रचना की गई जिसमें यदुनाथ सरकार ने शिवाजी एवं मराठा शक्ति का वर्णन किया है ।
इनकी... "मिलिटरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया" सन् 1960 ई . में प्रकाशित हुई ।
"हिस्ट्री ऑफ बंगाल", "इण्डिया आफ्टर इण्डिपेन्डेन्स" --भी इनकी अन्य रचनाएं हैं।
इसके साथ - साथ जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह ( द्वितीय ) के आग्रह पर इन्होंने जयपुर राज्य का इतिहास" द हिस्ट्री ऑफ जयपुर "की रचना की ।
आधुनिक काल के इतिहासकारों में विशेषकर उत्तर मध्यकालीन भारत का यदुनाथ सरकार ने जितना अच्छा अध्ययन करके प्रस्तुत किया उतना उनके बाद देखने को नहीं मिला..।
.अद्यतन इनकी पुण्यतिथि होने के साथ ही...इस वर्ष 150वीं जयन्ती भी है..इस अवसर पर ..... इतिहास का विद्यार्थी..उनको ..उनके कार्यों को स्मरण कर..स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है।
...इनका इतिहास लेखन मौलिक स्रोतों पर ही आधारित रहा है तथा इन पर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने प्रशस्ति में लिखा है-- कि वे भारत के महान इतिहासकार थे और उन्होंने मध्यकालीन भारत पर निष्ठापूर्वक कार्य किया है ।
--------
Pappusingh prajapat
अबूझमाड की शान - हांदावाड़ा जलप्रपात....!
बस्तर के झरनो मे चित्रकोट अौर तीरथगढ़ के बाद अगर सबसे प्रसिद्ध झरना है ,तो वो हैं हांदावाड़ा जलप्रपात. हांदावाड़ा झरने की खूबसुरती अौर विशालता ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया है , यहां जाने की चाहत के कारण , जितने भी बस्तर मे घुमने वाले लोग मिलते है वे सब मुझसे हांदावाड़ा झरने की जानकारी पुछते रहते है. सच मे यह बस्तर मे भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल साबित होगा. इसकी वजह इसकी खूबसूरती अौर विशालता के साथ साथ बारसूर से इसकी नजदीकी है.
बस्तर में दंतेवाड़ा जिले पर भी प्रकृति कम मेहरबान नहीं हैं. यहां दंतेवाड़ा में जहां घने जंगलो में ऊँची पर्वत चोटी पर गणेश जी विराजित हैं जहां प्रकृति एवँ इतिहास का अनूठा संगम दिखाई देता हैं वही विशालता लिये, सुन्दरतम झरना हांदावाड़ा जाने का मार्ग भी दंतेवाड़ा से ही जाता हैं. बस्तर में लोगो को दो जगह जाने की सबसे ज्यादा चाहत रहती हैं तो पहला हैं ढ़ोलकल और दुसरा हांदावाड़ा जलप्रपात.
हांदावाड़ा जलप्रपात नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड में आता हैं.जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से २० किलोमीटर की दुरी पर ऐतिहासिक नगरी बारसूर स्थित है. बारसूर से ०४ किलोमीटर की दुरी पर मूचनार नामक ग्राम में बस्तर की जीवनदायिनी इन्द्रावती बहती हैं. नदी के पार लगभग २५ से ३० किलोमीटर की दुरी पर अबूझमाड़ में हांदावाड़ा नाम का आधुनिक दुनिया से कटा हुआ छोटा सा ग्राम है. इस ग्राम से ०4 किलोमीटर की दुरी पर धारा डोंगरी की पहाड़ी में एक पहाड़ी नाला गोयदेर नदी लगभग 350 फ़ीट की ऊंचाई से गिरकर बहुत ही खूबसूरत एवं विशाल जलप्रपात का निर्माण करती है.
इसकी खूबसूरती इतनी मनमोहनी है की वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता है. बस एकटक देखते रहो. बहुत ही रोमांचक एवं मन को आन्दित करने का दृश्य कई दिनों तक आँखों के सामने से हटता ही नही हैं.बस वह मनमोहक दृश्य आँखों के सामने घूमता रहता है. जलप्रपात तक पहूँचने के लिये चार किलो मीटर के घने जंगल में पैदल चलना पड़ता हैं. जंगल बेहद घना एवँ डरावना हैं. गांव वालो की मदद के बिना यहां जाना असंभव एवँ खतरनाक हैं.
जलप्रपात की विशालता ,इसकी अप्रतिम सुन्दरता सारी थकान दूर कर देती हैं. इस जलप्रपात के ऊपर चढ़ने पर ऊपर एक छोटा सा झरना भी है। झरना छोटा है पर वो भी बहुत ही सुन्दर एवं मनमोहक है. झरने के ऊपर से चारो तरफ फैली हरियाली एवं निचे गिरता पानी की आवाज मन को बहुत ही आनंदित कर देते है.
इस झरने की आवाज 4 किलोमीटर की दुरी पर स्थित बस्ती में साफ साफ सुनाई देती है. बरसात के दिनों में यह जलप्रपात अपने विशाल रूप को पा लेता है. गर्मी के दिनों में नाले में पानी कम होने के कारन इसकी विशालता थोड़ी काम हो जाती है. वर्षाकाल में इन्द्रावती नदी अपने उफान पर होती है. इसलिए उस समय यहाँ पहुचना बहुत ही कष्ट दायक होता है.
नवम्बर से मार्च तक के समय इस झरने के पर्यटन का किया जा सकता है. यहाँ पहुचने के लिये पैदल जाना ही पड़ता है.पतली पगडण्डी में चलते हुए यहाँ पंहुचा जा सकता है. दोपहिया से अगर जाना हो तो मूचनार में इन्द्रावती नदी ,नाव में गाड़ी रख कर, नदी पार करके पगडंडी नुमा रास्तो से यहाँ पंहुचा जा सकता है. यहाँ जाने के लिए किसी जानकार व्यक्ति को साथ ले जाना उचित होगा.
आप हमे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं..!
बस्तर के झरनो मे चित्रकोट अौर तीरथगढ़ के बाद अगर सबसे प्रसिद्ध झरना है ,तो वो हैं हांदावाड़ा जलप्रपात. हांदावाड़ा झरने की खूबसुरती अौर विशालता ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया है , यहां जाने की चाहत के कारण , जितने भी बस्तर मे घुमने वाले लोग मिलते है वे सब मुझसे हांदावाड़ा झरने की जानकारी पुछते रहते है. सच मे यह बस्तर मे भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल साबित होगा. इसकी वजह इसकी खूबसूरती अौर विशालता के साथ साथ बारसूर से इसकी नजदीकी है.
बस्तर में दंतेवाड़ा जिले पर भी प्रकृति कम मेहरबान नहीं हैं. यहां दंतेवाड़ा में जहां घने जंगलो में ऊँची पर्वत चोटी पर गणेश जी विराजित हैं जहां प्रकृति एवँ इतिहास का अनूठा संगम दिखाई देता हैं वही विशालता लिये, सुन्दरतम झरना हांदावाड़ा जाने का मार्ग भी दंतेवाड़ा से ही जाता हैं. बस्तर में लोगो को दो जगह जाने की सबसे ज्यादा चाहत रहती हैं तो पहला हैं ढ़ोलकल और दुसरा हांदावाड़ा जलप्रपात.
हांदावाड़ा जलप्रपात नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड में आता हैं.जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से २० किलोमीटर की दुरी पर ऐतिहासिक नगरी बारसूर स्थित है. बारसूर से ०४ किलोमीटर की दुरी पर मूचनार नामक ग्राम में बस्तर की जीवनदायिनी इन्द्रावती बहती हैं. नदी के पार लगभग २५ से ३० किलोमीटर की दुरी पर अबूझमाड़ में हांदावाड़ा नाम का आधुनिक दुनिया से कटा हुआ छोटा सा ग्राम है. इस ग्राम से ०4 किलोमीटर की दुरी पर धारा डोंगरी की पहाड़ी में एक पहाड़ी नाला गोयदेर नदी लगभग 350 फ़ीट की ऊंचाई से गिरकर बहुत ही खूबसूरत एवं विशाल जलप्रपात का निर्माण करती है.
इसकी खूबसूरती इतनी मनमोहनी है की वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता है. बस एकटक देखते रहो. बहुत ही रोमांचक एवं मन को आन्दित करने का दृश्य कई दिनों तक आँखों के सामने से हटता ही नही हैं.बस वह मनमोहक दृश्य आँखों के सामने घूमता रहता है. जलप्रपात तक पहूँचने के लिये चार किलो मीटर के घने जंगल में पैदल चलना पड़ता हैं. जंगल बेहद घना एवँ डरावना हैं. गांव वालो की मदद के बिना यहां जाना असंभव एवँ खतरनाक हैं.
जलप्रपात की विशालता ,इसकी अप्रतिम सुन्दरता सारी थकान दूर कर देती हैं. इस जलप्रपात के ऊपर चढ़ने पर ऊपर एक छोटा सा झरना भी है। झरना छोटा है पर वो भी बहुत ही सुन्दर एवं मनमोहक है. झरने के ऊपर से चारो तरफ फैली हरियाली एवं निचे गिरता पानी की आवाज मन को बहुत ही आनंदित कर देते है.
इस झरने की आवाज 4 किलोमीटर की दुरी पर स्थित बस्ती में साफ साफ सुनाई देती है. बरसात के दिनों में यह जलप्रपात अपने विशाल रूप को पा लेता है. गर्मी के दिनों में नाले में पानी कम होने के कारन इसकी विशालता थोड़ी काम हो जाती है. वर्षाकाल में इन्द्रावती नदी अपने उफान पर होती है. इसलिए उस समय यहाँ पहुचना बहुत ही कष्ट दायक होता है.
नवम्बर से मार्च तक के समय इस झरने के पर्यटन का किया जा सकता है. यहाँ पहुचने के लिये पैदल जाना ही पड़ता है.पतली पगडण्डी में चलते हुए यहाँ पंहुचा जा सकता है. दोपहिया से अगर जाना हो तो मूचनार में इन्द्रावती नदी ,नाव में गाड़ी रख कर, नदी पार करके पगडंडी नुमा रास्तो से यहाँ पंहुचा जा सकता है. यहाँ जाने के लिए किसी जानकार व्यक्ति को साथ ले जाना उचित होगा.
आप हमे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं..!
बारसूर का युगल शिवालय - बत्तीसा मंदिर.....!
बस्तर के सभी शिवालयो मे बारसूर का युगल शिवालय वाला बत्तीसा मन्दिर मेरा सबसे प्रिय आराधना स्थल है। सिंहासन बत्तीसी में जहाँ बत्तीस पुतलिया जडी हुई थी वही इस मंदिर का मंडप बत्तीस स्तम्भो पर आधारित है जिसके कारण यह मंदिर बत्तीसा मन्दिर के नाम से ही जाना जाता है।
मंडप मे रखे हुए नन्दी पर शिल्पकार ने गजब की बारीक नक्काशी की। सुन्दर लड़वाली जंजीर पर लटकती घंटिया एकदम नयी सी लगती है। नन्दी महाराज के खुरो को इतने अच्छे तरीके से बनाया है जैसे बाहर की तरफ़ पैर मोड़ कर बैठा हुआ बछडा हो।
मन्दिर दो गर्भगृह युक्त है दोनो गर्भगृह में त्रिरथ शैली में निर्मित शिवलिंग स्थापित है। आकार प्रकार में बेहद आकर्षक एवं सुगठित है। इनकी एक अन्य विशेषता इन्हे सभी प्रस्तर शिवलिंग से अलग करती है। वह विशेषता है दोनों शिवलिंग का घुमना।ये ऐसे मात्र शिवलिंग है जिन्हे चारो ओर घुमाया जा सकता है. 800 सौ साल से ये शिवलिंग घुमाये जा रहे हैं।
ये दोनो शिवालय सोमेश्वर महादेव और गंगाधरेश्वर महादेव के नाम से शिलालेख में दर्ज है। सन 1208 में नाग शासन काल में राजमहिषी गंगमहादेवी ने यह मंदिर बनवाया था। एक शिवालय अपने नाम पर एवं दुसरा शिवालय अपने पति महाराज सोमेश्वर देव के नाम पर नामकरण किया।
मन्दिर के खर्च एवं रखरखाव के लिये केरुमर्क गाँव दान दिया था। तो फिर आईये कभी छत्तीसगढ़ के बारसूर....दंतेवाड़ा से कुल 30 किलोमीटर और गीदम से 20 किलोमीटर दुर इंद्रावती के तट पर बारसूर बसा है....!
.
बस्तर के सभी शिवालयो मे बारसूर का युगल शिवालय वाला बत्तीसा मन्दिर मेरा सबसे प्रिय आराधना स्थल है। सिंहासन बत्तीसी में जहाँ बत्तीस पुतलिया जडी हुई थी वही इस मंदिर का मंडप बत्तीस स्तम्भो पर आधारित है जिसके कारण यह मंदिर बत्तीसा मन्दिर के नाम से ही जाना जाता है।
मंडप मे रखे हुए नन्दी पर शिल्पकार ने गजब की बारीक नक्काशी की। सुन्दर लड़वाली जंजीर पर लटकती घंटिया एकदम नयी सी लगती है। नन्दी महाराज के खुरो को इतने अच्छे तरीके से बनाया है जैसे बाहर की तरफ़ पैर मोड़ कर बैठा हुआ बछडा हो।
मन्दिर दो गर्भगृह युक्त है दोनो गर्भगृह में त्रिरथ शैली में निर्मित शिवलिंग स्थापित है। आकार प्रकार में बेहद आकर्षक एवं सुगठित है। इनकी एक अन्य विशेषता इन्हे सभी प्रस्तर शिवलिंग से अलग करती है। वह विशेषता है दोनों शिवलिंग का घुमना।ये ऐसे मात्र शिवलिंग है जिन्हे चारो ओर घुमाया जा सकता है. 800 सौ साल से ये शिवलिंग घुमाये जा रहे हैं।
ये दोनो शिवालय सोमेश्वर महादेव और गंगाधरेश्वर महादेव के नाम से शिलालेख में दर्ज है। सन 1208 में नाग शासन काल में राजमहिषी गंगमहादेवी ने यह मंदिर बनवाया था। एक शिवालय अपने नाम पर एवं दुसरा शिवालय अपने पति महाराज सोमेश्वर देव के नाम पर नामकरण किया।
मन्दिर के खर्च एवं रखरखाव के लिये केरुमर्क गाँव दान दिया था। तो फिर आईये कभी छत्तीसगढ़ के बारसूर....दंतेवाड़ा से कुल 30 किलोमीटर और गीदम से 20 किलोमीटर दुर इंद्रावती के तट पर बारसूर बसा है....!
.