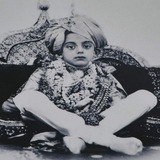कूटे जो है.... मूसर...!
मूसर से शायद ही कोई अपरिचित हो.ये बहुत पुराने समय से घरों में आनाज कुटाई का प्रमुख यंत्र रहा है.साथ ही आनाज छड़ने का काम भी होता है.छड़ना यानी कि सफाई करना.दरअसल कई बार चावल में धान के अंश रह जाते हैं.उसकी सफाई इसी से होती है.साथ ही मक्का,मंडिया,कोदो,कोसरा आदि बीज के ऊपर एक हल्की सी परत होती है.जिसे मूसर से ही छड़कर अलग किया जाता है.
मूसर सभी जगह ये इसी नाम से जाना जाता है.हिन्दी में इस पर मुहावरे और लोकोत्तियाँ भी प्रचलित हैं-जैसे मूसलाधार वर्षा होना,ओखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना....आदि.
मूसल की लंबाई लगभग 80 से 90 से.मी. तक की होती है.यह लम्बा-अंडाकार होता है.नीचे बने एक गोल वलय होता है ताकि हाथ ऊपर न फिसले और नीचे बने हत्थे को मजबूती से पकड़ा जा सके.हत्थे के नीचे लोहे का मूसलाधार लगा होता है.जो 4-5 से.मी. तक लंबा लोहे का बना रिंग होता है.ये रिंग "साम" कहलाता है.इसका वजन 1 से 1.5 कि.ग्रा. तक का होता है.
कोटेन=कुटाई के लिए भूमि पर एक छिद्र बना होता है,जिसे कोटेन सा बाहना कहा जाता है.लकड़ी पर लगभग 7-8 से.मी. व्यास और लगभग इतनी ही गहराई का छिद्र बनाकर जमीन पर स्थाई रूप से स्थापित कर दिया जाता.यही कोटेन/बाहना है.
होली के अवसर पर एक मजाकिया गीत भी गाया जाता है-"मूसर कूटे बाहना में,तोर डवकी ल दे दे गाहना में"
मूसर के बगैर बस्तर के कई रिवाज जैसे अधूरे हैं.
चिवड़ा/लाई के बगैर नवाखाई का पर्व या माहला/सगाई की रस्म संभव ही नहीं है.जो मूसल से ही तैयार होता है.चिवड़ा लाई की कुटाई में प्रयुक्त होने वाले मूसर में लोहे का आधार(साम)नहीं होता.
बस्तर में नए शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद औरतें घर-घर "तिल कोंडा"(तिल-गुड़ का प्रसाद)वितरित करते हैं.इसे महिलाएँ,लड़कियाँ या छोटे बच्चे ही खा सकते हैं.इस मीठे "तिल कोंडा"की कुटाई मूसर से ही होती है.
मूसर के बगैर विवाह की रस्म भी अधूरी है.क्योंकि विवाह के अवसर पर दुल्हा-दुल्हन को चढ़ाई जाने वाले घरेलू हल्दी की कुटाई भी मूसल से होती है.सुंदर गीत गाती हुई "हरदी कूटनी" की ये रस्म गाँव के पुजारी या गाँयता परिवार की महिलाएँ व गाँव की लड़कियाँ सम्पन्न करती हैं.
कुटाई के दौरान मूसर का हत्था एक हाथ की मुट्ठी में होता है.दूसरे हाथ ही ऊँगलियों से कोटेन के आनाज को संभाला जाता है.ताकि आनाज यत्र-तत्र न बिखर जाएँ.कुटाई के दौरान एक पैर को जमीन को जमीन पर सीधा रखने व दूसरे पैर के को मोड़ा जाता है.फिर थोड़ा सिर नीचे झुककर आनाज की कुटाई की जाती है.भारी मूसर का एक हाथ से संतुलन बनाना कोेटेने में निशाना साधना बड़ा मुश्किल काम होता है.
लेकिन औरतें धान कुटाई में इतनी अभ्यस्त हैं कि वे आँख मूदकर भी ये काम बड़ी आसानी से कर सकती हैं.मूसर की कुटाई से बने कनकी पेज या जोंधरा पेज पीकर आनंद आ जाता है.कभी सवरे-सवेरे मूसर की कुटाई की "ढुक-ढुक" की आवाज सुनिएगा तन-मन को आनंद से भर जाएगा.
हमारी माँ सूर्यग्रहण के समय इसे थाली पर सीधा-खड़ा छोड़ देती है,यह आश्चर्यजनक रूप से स्तंभ की भाँति खड़ा रहता है.आपने भी ये चमत्कार जरुर देखा होगा.
अशोक कुमार नेताम
आप हमे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं..!
मूसर से शायद ही कोई अपरिचित हो.ये बहुत पुराने समय से घरों में आनाज कुटाई का प्रमुख यंत्र रहा है.साथ ही आनाज छड़ने का काम भी होता है.छड़ना यानी कि सफाई करना.दरअसल कई बार चावल में धान के अंश रह जाते हैं.उसकी सफाई इसी से होती है.साथ ही मक्का,मंडिया,कोदो,कोसरा आदि बीज के ऊपर एक हल्की सी परत होती है.जिसे मूसर से ही छड़कर अलग किया जाता है.
मूसर सभी जगह ये इसी नाम से जाना जाता है.हिन्दी में इस पर मुहावरे और लोकोत्तियाँ भी प्रचलित हैं-जैसे मूसलाधार वर्षा होना,ओखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना....आदि.
मूसल की लंबाई लगभग 80 से 90 से.मी. तक की होती है.यह लम्बा-अंडाकार होता है.नीचे बने एक गोल वलय होता है ताकि हाथ ऊपर न फिसले और नीचे बने हत्थे को मजबूती से पकड़ा जा सके.हत्थे के नीचे लोहे का मूसलाधार लगा होता है.जो 4-5 से.मी. तक लंबा लोहे का बना रिंग होता है.ये रिंग "साम" कहलाता है.इसका वजन 1 से 1.5 कि.ग्रा. तक का होता है.
कोटेन=कुटाई के लिए भूमि पर एक छिद्र बना होता है,जिसे कोटेन सा बाहना कहा जाता है.लकड़ी पर लगभग 7-8 से.मी. व्यास और लगभग इतनी ही गहराई का छिद्र बनाकर जमीन पर स्थाई रूप से स्थापित कर दिया जाता.यही कोटेन/बाहना है.
होली के अवसर पर एक मजाकिया गीत भी गाया जाता है-"मूसर कूटे बाहना में,तोर डवकी ल दे दे गाहना में"
मूसर के बगैर बस्तर के कई रिवाज जैसे अधूरे हैं.
चिवड़ा/लाई के बगैर नवाखाई का पर्व या माहला/सगाई की रस्म संभव ही नहीं है.जो मूसल से ही तैयार होता है.चिवड़ा लाई की कुटाई में प्रयुक्त होने वाले मूसर में लोहे का आधार(साम)नहीं होता.
बस्तर में नए शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद औरतें घर-घर "तिल कोंडा"(तिल-गुड़ का प्रसाद)वितरित करते हैं.इसे महिलाएँ,लड़कियाँ या छोटे बच्चे ही खा सकते हैं.इस मीठे "तिल कोंडा"की कुटाई मूसर से ही होती है.
मूसर के बगैर विवाह की रस्म भी अधूरी है.क्योंकि विवाह के अवसर पर दुल्हा-दुल्हन को चढ़ाई जाने वाले घरेलू हल्दी की कुटाई भी मूसल से होती है.सुंदर गीत गाती हुई "हरदी कूटनी" की ये रस्म गाँव के पुजारी या गाँयता परिवार की महिलाएँ व गाँव की लड़कियाँ सम्पन्न करती हैं.
कुटाई के दौरान मूसर का हत्था एक हाथ की मुट्ठी में होता है.दूसरे हाथ ही ऊँगलियों से कोटेन के आनाज को संभाला जाता है.ताकि आनाज यत्र-तत्र न बिखर जाएँ.कुटाई के दौरान एक पैर को जमीन को जमीन पर सीधा रखने व दूसरे पैर के को मोड़ा जाता है.फिर थोड़ा सिर नीचे झुककर आनाज की कुटाई की जाती है.भारी मूसर का एक हाथ से संतुलन बनाना कोेटेने में निशाना साधना बड़ा मुश्किल काम होता है.
लेकिन औरतें धान कुटाई में इतनी अभ्यस्त हैं कि वे आँख मूदकर भी ये काम बड़ी आसानी से कर सकती हैं.मूसर की कुटाई से बने कनकी पेज या जोंधरा पेज पीकर आनंद आ जाता है.कभी सवरे-सवेरे मूसर की कुटाई की "ढुक-ढुक" की आवाज सुनिएगा तन-मन को आनंद से भर जाएगा.
हमारी माँ सूर्यग्रहण के समय इसे थाली पर सीधा-खड़ा छोड़ देती है,यह आश्चर्यजनक रूप से स्तंभ की भाँति खड़ा रहता है.आपने भी ये चमत्कार जरुर देखा होगा.
अशोक कुमार नेताम
आप हमे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं..!
तृणराज /सदाफल
----------------------
भारत के प्रमुख फल..'नारियल' ...जिसका भारत में आनुष्ठानिक महत्त्व अधिक है -- का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य शक नहपान के दामाद ऋषभदत्त के नासिक गुहा अभिलेख (123 ई. ) से मिलता है ।
पुरातात्त्विक रूप से , पहली शती ई.पू. में -- पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी के निकट अरिकामेडु में जूट की रस्सी के रूप में , नारियल की उपस्थिति का संकेत प्राचीनतम रूप में मिलता है ।
दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त , नारियल - फलक का परिचय होना भारत के समुद्रतटीय भू - भागों के लिए पेड़ का बहुविध उपयोग एक बड़ी आर्थिक घटना थी ... क्योंकि , खासतौर से इसका फल और रेशे ( नारियल जटा ) के साथ साथ लकड़ी का भी उपयोग किया जा सकता था । नारियल जटा भारतीय समुद्र में ज्यादातर जहाजों के पटरों को बिछाने के साथ बाँधने के काम आती थी तथा यह सिलसिला लगभग एक हज़ार साल तक यानि सोलहवीं शती के आरम्भ तक चलता रहा।
14वीं शती ई . के यात्री इब्नबतूता ने नारियल का रोचक विवरण दिया है--
" ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक हैं । ये हू - बहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं । इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के-- एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर । नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है क्योंकि इसमें भी मानो दो आँखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है । वे इससे रस्सी बनाते हैं । लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज़ को सिलते हैं ...वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं ।"
-------
Pappusingh prajapat
----------------------
भारत के प्रमुख फल..'नारियल' ...जिसका भारत में आनुष्ठानिक महत्त्व अधिक है -- का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य शक नहपान के दामाद ऋषभदत्त के नासिक गुहा अभिलेख (123 ई. ) से मिलता है ।
पुरातात्त्विक रूप से , पहली शती ई.पू. में -- पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी के निकट अरिकामेडु में जूट की रस्सी के रूप में , नारियल की उपस्थिति का संकेत प्राचीनतम रूप में मिलता है ।
दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त , नारियल - फलक का परिचय होना भारत के समुद्रतटीय भू - भागों के लिए पेड़ का बहुविध उपयोग एक बड़ी आर्थिक घटना थी ... क्योंकि , खासतौर से इसका फल और रेशे ( नारियल जटा ) के साथ साथ लकड़ी का भी उपयोग किया जा सकता था । नारियल जटा भारतीय समुद्र में ज्यादातर जहाजों के पटरों को बिछाने के साथ बाँधने के काम आती थी तथा यह सिलसिला लगभग एक हज़ार साल तक यानि सोलहवीं शती के आरम्भ तक चलता रहा।
14वीं शती ई . के यात्री इब्नबतूता ने नारियल का रोचक विवरण दिया है--
" ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक हैं । ये हू - बहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं । इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के-- एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर । नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है क्योंकि इसमें भी मानो दो आँखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है । वे इससे रस्सी बनाते हैं । लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज़ को सिलते हैं ...वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं ।"
-------
Pappusingh prajapat
छिन्द में छुपा है बस्तर.....!
बस्तर में लगभग सब जगह छिन्द के पेड़ आपको दिखाई देंगे। यह खजुर की पेड़ की ही एक उप प्रजाति है। किन्तु खजुर से अलग है। यह पेड़ पांच फीट से चालीस फीट तक का ऊँचा होता है। मई के अंत में ये फल लगने लग जाते है। बस्तर में इस फल को छिन्दपाक कहा जाता है। अभी पुरे बस्तर के छिन्द पेड़ में छिन्दपाक लगे हुए है।
फल लगने से लेकर पकने तक ये फल तीन बार अपना रंग बदलते है, शुरूआत में हरा , मध्य में स्वर्ण की तरह पीला , और पकने पर भूरे कथ्थई रंग के हो जाते है। अभी कहीं कहीं छिन्द के फल पीले हो चुके है , जब सूर्य की रोशनी इन पीले छिन्द के गुच्छो पर पड़ती है तब ये फल सोने से बने फल जैसे लगते है। कहीं कहीं छिन्द पाक पक कर बाजारो में आ चुके है। यह मीठा एवं खजुर की तरह होता है पर खजुर से भिन्न होता है। खजुर का आकार बड़ा होता है इसका आकार छोटा होता है। सुखने पर इसका खारक नहीं बनता है। छिन्द पाक को खाने से पानी प्यास बहुत लगती है। इसे सुखा कर भी रखा जाता है ताकि वर्ष भर खाया जा सके।
छिन्द का बस्तर से शुरू से ही गहरा नाता है. यह मात्र एक संयोग ही है बस्तर में नौवी सदी से तेरहवी सदी तक शासन करने वाले , ज़िनके बनाये मन्दिर , तालाब आज बस्तर की ऐतिहासिक पहचान है उस छिन्दक नागवंश एवं छिन्द पेड़ में आज नाम की साम्यता दिखाई देती है।
वही दुसरी ओर बस्तर में बहुत से गांवो के नाम में छिन्द का होना भी बस्तर की एक अनोखी विशेषता है। भले ही गांव का नाम छिन्दनार हो या छिन्दगांव , या छिन्दगढ़ , छिन्दबहार हो या छिन्दगुफा , इन सभी मे छिन्द नाम जुड़ा होना भी बस्तर का छिन्द से गहरे नाते को दिखाता है।
इंस्टाग्राम में हमें जरूर फालो कीजिये।
https://www.instagram.com/bastar_bhushan
बस्तर में लगभग सब जगह छिन्द के पेड़ आपको दिखाई देंगे। यह खजुर की पेड़ की ही एक उप प्रजाति है। किन्तु खजुर से अलग है। यह पेड़ पांच फीट से चालीस फीट तक का ऊँचा होता है। मई के अंत में ये फल लगने लग जाते है। बस्तर में इस फल को छिन्दपाक कहा जाता है। अभी पुरे बस्तर के छिन्द पेड़ में छिन्दपाक लगे हुए है।
फल लगने से लेकर पकने तक ये फल तीन बार अपना रंग बदलते है, शुरूआत में हरा , मध्य में स्वर्ण की तरह पीला , और पकने पर भूरे कथ्थई रंग के हो जाते है। अभी कहीं कहीं छिन्द के फल पीले हो चुके है , जब सूर्य की रोशनी इन पीले छिन्द के गुच्छो पर पड़ती है तब ये फल सोने से बने फल जैसे लगते है। कहीं कहीं छिन्द पाक पक कर बाजारो में आ चुके है। यह मीठा एवं खजुर की तरह होता है पर खजुर से भिन्न होता है। खजुर का आकार बड़ा होता है इसका आकार छोटा होता है। सुखने पर इसका खारक नहीं बनता है। छिन्द पाक को खाने से पानी प्यास बहुत लगती है। इसे सुखा कर भी रखा जाता है ताकि वर्ष भर खाया जा सके।
छिन्द का बस्तर से शुरू से ही गहरा नाता है. यह मात्र एक संयोग ही है बस्तर में नौवी सदी से तेरहवी सदी तक शासन करने वाले , ज़िनके बनाये मन्दिर , तालाब आज बस्तर की ऐतिहासिक पहचान है उस छिन्दक नागवंश एवं छिन्द पेड़ में आज नाम की साम्यता दिखाई देती है।
वही दुसरी ओर बस्तर में बहुत से गांवो के नाम में छिन्द का होना भी बस्तर की एक अनोखी विशेषता है। भले ही गांव का नाम छिन्दनार हो या छिन्दगांव , या छिन्दगढ़ , छिन्दबहार हो या छिन्दगुफा , इन सभी मे छिन्द नाम जुड़ा होना भी बस्तर का छिन्द से गहरे नाते को दिखाता है।
इंस्टाग्राम में हमें जरूर फालो कीजिये।
https://www.instagram.com/bastar_bhushan
The lost sun temple of Multan
-------------------------------------------------
.मुल्तान बहुत प्राचीन नगर है । सिकंदर के भारत में आने के समय वह नगर ‘ मार्हन्स ' जाति की राजधानी
था । जनरल कनिंगम साहब की सम्मति में ' सूर्य - भगवान् ' के मंदिर के कारण इसकी प्रसिद्धि हुई ।
कहा जाता है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब का कुष्ठ रोग ...इस स्थान पर सूर्योपासना के कारण जाता रहा।
भविष्य पुराण के कथन की पुष्टि में आर.जी. भण्डारकर ने यह मत दिया कि - ' कृष्ण के पुत्र
साम्ब ने शक द्वीप ( सिस्तान ) के ' मग ' नामक ईरानी ' पुरोहितों को भारत में लाकर सूर्य - पूजा को प्रचलित करवाया ।
उन्होंने पंजाब में चंद्रभागा नदी पर ' मूलस्थान ' ( मुल्तान ) नामक नगर का निर्माण कर , साम्ब द्वारा यहाँ निर्मित प्रथम सूर्य मन्दिर में पूर्जा - अर्चना की । उनके द्वारा सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में ' शम्बपुरायात्रोत्सव ' मनाया जाता है । गोविन्दपुर लेख ( गया ,बिहार 1137 ई . ) में मग्ग ब्राह्मणों का विस्तृत वर्णन मिलता है ।
ह्वेनसांग भी मूलस्थान ' ( मुल्तान ) के साम्ब द्वारा निर्मित सूर्य मन्दिर का विवरण देता है जिसकी मूर्ति सोने की थी । वृहत्संहिता में भी ईरानी प्रभाव वाली सूर्य पूजा को मगों द्वारा भारत में प्रचलित करने का वर्णन है । अलबरूनी भी मगों को
सूर्य का सच्चा पुजारी कहता है ।
बिलादुरी भी ( 875 ई . ) में इस मूर्ति का वर्णन करते हुए लिखता है कि समस्त सिंधु - प्रान्त के यात्री यहाँ आकर सिर तथा दाढ़ी इत्यादि मुँडा मंदिर की परिक्रमा करते हैं । अबूज़ैद तथा अलमसूदी ने भी ( 920 ई . ) में इसका वर्णन किया है । इब्न हौकल ( 976 ई . ) का कथन है कि एक पुरुषाकार मूर्ति वेदी पर बनी हुई थी । इसकी आँखों में हीरे लगे हुए थे और शरीर रक्त चर्म से आच्छादित था । यह पता नहीं चलता कि यह मूर्ति किस वस्तु से बनायी गई थी । इब्न हौकल के कुछ काल पश्चात् ' करामतह ' ने इस नगर को जीत लिया और मूर्ति तोड़कर उस स्थान में एक मस्जिद बनवा दी । अलबरुनी के समय यह मूर्ति न थी । औरंगजेब के राज्यकाल में एक फ्रांसीसी यात्री यहाँ आया था और उसका भी इस मूर्ति के सम्बन्ध में दिया हुआ वर्णन इब्न हौक़ल के वर्णन से ठीक मिलता है ।
जनरल कनिंगम साहब ने इसके खंडहर ( सन् 1853 में ) खुदवा कर देखे थे और वह गढ़ के मध्यभाग में मिले जिससे पश्चिमी यात्रियों के इस कथन की पुष्टि होती है कि मंदिर बाजार के मध्य में बना हुआ था । बहुत संभव है कि नगर से पाँच मील दूर बने हुए वर्तमान ' सूर्यकुंड ' का इस मंदिर से कुछ सम्बन्ध हो ।
----
Pappusingh prajapat
-------------------------------------------------
.मुल्तान बहुत प्राचीन नगर है । सिकंदर के भारत में आने के समय वह नगर ‘ मार्हन्स ' जाति की राजधानी
था । जनरल कनिंगम साहब की सम्मति में ' सूर्य - भगवान् ' के मंदिर के कारण इसकी प्रसिद्धि हुई ।
कहा जाता है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब का कुष्ठ रोग ...इस स्थान पर सूर्योपासना के कारण जाता रहा।
भविष्य पुराण के कथन की पुष्टि में आर.जी. भण्डारकर ने यह मत दिया कि - ' कृष्ण के पुत्र
साम्ब ने शक द्वीप ( सिस्तान ) के ' मग ' नामक ईरानी ' पुरोहितों को भारत में लाकर सूर्य - पूजा को प्रचलित करवाया ।
उन्होंने पंजाब में चंद्रभागा नदी पर ' मूलस्थान ' ( मुल्तान ) नामक नगर का निर्माण कर , साम्ब द्वारा यहाँ निर्मित प्रथम सूर्य मन्दिर में पूर्जा - अर्चना की । उनके द्वारा सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में ' शम्बपुरायात्रोत्सव ' मनाया जाता है । गोविन्दपुर लेख ( गया ,बिहार 1137 ई . ) में मग्ग ब्राह्मणों का विस्तृत वर्णन मिलता है ।
ह्वेनसांग भी मूलस्थान ' ( मुल्तान ) के साम्ब द्वारा निर्मित सूर्य मन्दिर का विवरण देता है जिसकी मूर्ति सोने की थी । वृहत्संहिता में भी ईरानी प्रभाव वाली सूर्य पूजा को मगों द्वारा भारत में प्रचलित करने का वर्णन है । अलबरूनी भी मगों को
सूर्य का सच्चा पुजारी कहता है ।
बिलादुरी भी ( 875 ई . ) में इस मूर्ति का वर्णन करते हुए लिखता है कि समस्त सिंधु - प्रान्त के यात्री यहाँ आकर सिर तथा दाढ़ी इत्यादि मुँडा मंदिर की परिक्रमा करते हैं । अबूज़ैद तथा अलमसूदी ने भी ( 920 ई . ) में इसका वर्णन किया है । इब्न हौकल ( 976 ई . ) का कथन है कि एक पुरुषाकार मूर्ति वेदी पर बनी हुई थी । इसकी आँखों में हीरे लगे हुए थे और शरीर रक्त चर्म से आच्छादित था । यह पता नहीं चलता कि यह मूर्ति किस वस्तु से बनायी गई थी । इब्न हौकल के कुछ काल पश्चात् ' करामतह ' ने इस नगर को जीत लिया और मूर्ति तोड़कर उस स्थान में एक मस्जिद बनवा दी । अलबरुनी के समय यह मूर्ति न थी । औरंगजेब के राज्यकाल में एक फ्रांसीसी यात्री यहाँ आया था और उसका भी इस मूर्ति के सम्बन्ध में दिया हुआ वर्णन इब्न हौक़ल के वर्णन से ठीक मिलता है ।
जनरल कनिंगम साहब ने इसके खंडहर ( सन् 1853 में ) खुदवा कर देखे थे और वह गढ़ के मध्यभाग में मिले जिससे पश्चिमी यात्रियों के इस कथन की पुष्टि होती है कि मंदिर बाजार के मध्य में बना हुआ था । बहुत संभव है कि नगर से पाँच मील दूर बने हुए वर्तमान ' सूर्यकुंड ' का इस मंदिर से कुछ सम्बन्ध हो ।
----
Pappusingh prajapat
"एक रात लगातार बारिश हुई..यह आश्चर्य की बात है कि जहां अन्य दिनों में सारस का जोड़ा अंडों पर बारी - बारी से 5 या 6 बार बैठता था , इस दौरान जब रात और दिन बारिश हो रही थी और हवा अपेक्षाकृत ठंडी हो चली थी , अंडों पर नर सारस.. भोर से लेकर आधे दिन तक निरन्तर बैठा रहता था और मादा सारस .. इस समय से ( आधे दिन से ) लेकर अगले दिन सुबह तक बिना व्यवधान के अंडों पर बैठी रहती थी , ताकि -- अंडों को गर्म रखा जा सके । इस डर के कारण कि कहीं एक के द्वारा अंडे छोड़ने और दूसरे के द्वारा अंडों पर जल्दी - जल्दी बैठने के दौरान हवा की ठंडक का कुछ असर हो सकता है और अंडे कुछ नमी पकड़ सकते हैं , जो उन्हें नष्ट कर सकती है ।
इससे पता चलता है कि मनुष्य -- समझ ( ज्ञान , विवेक ) बुद्धि द्वारा प्राप्त करता है जबकि पशु ( पक्षी ) ... इसे ( ज्ञान ) प्राकृतिक प्रज्ञा ( दैवी प्रेरणा ) से प्राप्त करते हैं ।
यह आश्चर्यजनक था कि शुरुआती दिनों में , अंडे सेने वाला पक्षी अंडों को अपने सीने के पास लगाकर रखता था । चौदह - पन्द्रह दिनों के बाद , इस डर से कि बहुत पास रहने से तापमान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने और अत्यधिक गर्मी से अंडे नष्ट हो सकते हैं , अंडों को ( बैठने वाला पक्षी ) सीने से कुछ दूरी पर रखता ।"
--सारस का एक जोड़ा ..जो स्वयं जहांगीर द्वारा पाला गया था.1619 में जब वह अहमदाबाद ,गुजरात में था ..तब का यह विवरण ( तुजुक ए जहांगीरी )।
इससे हम ये जान सकते हैं कि जहांगीर...पशु पक्षियों का सूक्ष्म अवलोकन करता था...
अपने इसी प्रकृत प्रेम के कारण उसने अपने दरबारी चित्रकार मंसूर से विभिन्न पक्षियों के चित्र बनवाए--
मंसूर द्वारा बनाया गया ..साइबेरियन सारस का एक चित्र👇
इससे पता चलता है कि मनुष्य -- समझ ( ज्ञान , विवेक ) बुद्धि द्वारा प्राप्त करता है जबकि पशु ( पक्षी ) ... इसे ( ज्ञान ) प्राकृतिक प्रज्ञा ( दैवी प्रेरणा ) से प्राप्त करते हैं ।
यह आश्चर्यजनक था कि शुरुआती दिनों में , अंडे सेने वाला पक्षी अंडों को अपने सीने के पास लगाकर रखता था । चौदह - पन्द्रह दिनों के बाद , इस डर से कि बहुत पास रहने से तापमान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने और अत्यधिक गर्मी से अंडे नष्ट हो सकते हैं , अंडों को ( बैठने वाला पक्षी ) सीने से कुछ दूरी पर रखता ।"
--सारस का एक जोड़ा ..जो स्वयं जहांगीर द्वारा पाला गया था.1619 में जब वह अहमदाबाद ,गुजरात में था ..तब का यह विवरण ( तुजुक ए जहांगीरी )।
इससे हम ये जान सकते हैं कि जहांगीर...पशु पक्षियों का सूक्ष्म अवलोकन करता था...
अपने इसी प्रकृत प्रेम के कारण उसने अपने दरबारी चित्रकार मंसूर से विभिन्न पक्षियों के चित्र बनवाए--
मंसूर द्वारा बनाया गया ..साइबेरियन सारस का एक चित्र👇
सिक्कों की पहचान का लुप्त ग्रंथ : रूपसूत्र
#अतीत_आख्यान
*श्रीकृष्ण "जुगनू"
प्राचीन काल में जबकि अलग- अलग इलाकों में अलग-अलग सिक्कों का व्यवहार था, तब सिक्कों के मानक रूप, उनके ऊपर अंकित चिह्नों के अभिप्राय, उनके प्रचलन इलाकों और उन इलाकों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देने वाला एक ग्रंथ था : रूपसूत्र। आज यह ग्रंथ हम खो चुके हैं और इसकी जानकारी तक हमें नहीं होती यदि बुद्धघोष इसका उल्लेख नहीं करता।
'रूप' शब्द का प्रयोग मूर्ति के अर्थ में मध्यकाल में मिलता है क्योंकि सूत्रधार मंडन ने 1450 ईस्वी में 'रूपमंडन' और सूत्रधार नाथा ने 1480 में "रूपाधिकार" नाम से मूर्तिकला पर ग्रंथ रचे। (वास्तुमंजरी : नाथाकृत, संपादक श्रीकृष्ण जुगनू) हालांकि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने रूप शब्द का प्रयोग बताया है ( 5, 2, 120) तथा उससे बने 'रूप्य' शब्द का अभिप्राय 'सुंदर' एवं 'आहत' यानी मुहर युक्त बताया है। यही शब्द बाद में सिक्के के लिए चलन में आया क्योंकि अर्थशास्त्र ने रूप का अर्थ सिक्का ही लिया है और न केवल चांदी बल्कि तांबे के सिक्के के लिए भी यही प्रयोग किया है - 'रूप्यारूप' एवं 'ताम्ररूप'। पतंजलि ने 'रूपतके' शब्द का प्रयोग पाणिनि के एक सूत्र (1, 4, 52) के वार्त्तिक के प्रसंग में किया है जो कार्षापणों की जांच करता था। चाणक्य ने इस पदाधिकारी के लिए 'रूपदर्शक' शब्द का प्रयोग किया है।
प्राचीन काल में सिक्कों के ढालने व चलाने के लिए प्राविधिक मुद्राशास्त्र था जिसकी ओर संकेत लेखक बुद्धघोष ने अपनी "समंतपासादिका" में किया है। तब अजातशत्रु या बिंबिसार के 20 माषक का कार्षापणों का चलन था और उसे नीलकाहापण नाम बुद्धघोष ने दिया था। उस समय सिक्कों के निरीक्षण का काम बड़ी जिम्मेदारी से किया जाता था। एेसे दायित्वबोध की चर्चा के साथ ही कौटिल्य ने 'लक्षणाध्यक्ष' नामक टकसाल के अधिकारी का उल्लेख किया है। उसके साथ जांच का काम 'रूपदर्शक' करता था। वह जांचकर बार बार सिक्कों पर मुहर लगाता जाता था। एेसी लगभग एक दर्जन मुहरों वाले सिक्के अब तक मिल चुके हैं और अधिक संख्या वाले घिस-पिट चुके हैं।
इस सिक्कों पर लगाये गए प्रतीकों और चिह्नों का पूरा अर्थ होता था जिसे आज अनुमान से ही जाना गया है जबकि बुद्धघोष का कहना है कि "रूपसूत्र" में इसका विवरण मिल जाता था। इस ग्रंथ का अभ्यासी "हेरञ्जक" कहलाता था और वह चित्र-विचित्र सिक्के देखकर निम्न बातें कह सकता था :
1. कोई सिक्का किस गांव, निगम या राजधानी है ?
2. सिक्का किस टकसाल में ढाला गया है ?
3. उसका मूल्य व धातु क्या-क्या है ?
यही नहीं, हेरञ्जक यह भी बता सकता था कि सिक्कों वाला गांव, निगम आदि किस दिशा, पहाड़ी के शिखर या नदी के तट पर मौजूद है। ( Bhudhhistic studies p. 432)
है न रोचक किताब की बात। यह पुस्तक कीमती इसलिये थी कि उसके अभ्यास से सिक्कों की पहचान करते-करते आंखें खोने का भय नहीं रहता था। इसीलिये सर्राफ लोग भी उसका अभ्यास करते थे। क्या यह ग्रंथ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व विद्यालयों में पढ़ाया जाता था ?
मुझे तो मालूम नहीं मगर यह ग्रंथ एक आवश्यकता थी, यह एक प्रमाण की उपज था और इसी आवश्यता ने बाद में मुद्राशास्त्र को जन्म दिया लेकिन क्या हम वह "रूपसूत्र" लौटा सके ? आप इस कुंजी के बारे क्या जानते हैं, जरूर बताइयेगा।
जय-जय।
( रिपोस्ट)
(मित्रों से अधिकाधिक शेयर करने का आग्रह है)
#अतीत_आख्यान
*श्रीकृष्ण "जुगनू"
प्राचीन काल में जबकि अलग- अलग इलाकों में अलग-अलग सिक्कों का व्यवहार था, तब सिक्कों के मानक रूप, उनके ऊपर अंकित चिह्नों के अभिप्राय, उनके प्रचलन इलाकों और उन इलाकों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देने वाला एक ग्रंथ था : रूपसूत्र। आज यह ग्रंथ हम खो चुके हैं और इसकी जानकारी तक हमें नहीं होती यदि बुद्धघोष इसका उल्लेख नहीं करता।
'रूप' शब्द का प्रयोग मूर्ति के अर्थ में मध्यकाल में मिलता है क्योंकि सूत्रधार मंडन ने 1450 ईस्वी में 'रूपमंडन' और सूत्रधार नाथा ने 1480 में "रूपाधिकार" नाम से मूर्तिकला पर ग्रंथ रचे। (वास्तुमंजरी : नाथाकृत, संपादक श्रीकृष्ण जुगनू) हालांकि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने रूप शब्द का प्रयोग बताया है ( 5, 2, 120) तथा उससे बने 'रूप्य' शब्द का अभिप्राय 'सुंदर' एवं 'आहत' यानी मुहर युक्त बताया है। यही शब्द बाद में सिक्के के लिए चलन में आया क्योंकि अर्थशास्त्र ने रूप का अर्थ सिक्का ही लिया है और न केवल चांदी बल्कि तांबे के सिक्के के लिए भी यही प्रयोग किया है - 'रूप्यारूप' एवं 'ताम्ररूप'। पतंजलि ने 'रूपतके' शब्द का प्रयोग पाणिनि के एक सूत्र (1, 4, 52) के वार्त्तिक के प्रसंग में किया है जो कार्षापणों की जांच करता था। चाणक्य ने इस पदाधिकारी के लिए 'रूपदर्शक' शब्द का प्रयोग किया है।
प्राचीन काल में सिक्कों के ढालने व चलाने के लिए प्राविधिक मुद्राशास्त्र था जिसकी ओर संकेत लेखक बुद्धघोष ने अपनी "समंतपासादिका" में किया है। तब अजातशत्रु या बिंबिसार के 20 माषक का कार्षापणों का चलन था और उसे नीलकाहापण नाम बुद्धघोष ने दिया था। उस समय सिक्कों के निरीक्षण का काम बड़ी जिम्मेदारी से किया जाता था। एेसे दायित्वबोध की चर्चा के साथ ही कौटिल्य ने 'लक्षणाध्यक्ष' नामक टकसाल के अधिकारी का उल्लेख किया है। उसके साथ जांच का काम 'रूपदर्शक' करता था। वह जांचकर बार बार सिक्कों पर मुहर लगाता जाता था। एेसी लगभग एक दर्जन मुहरों वाले सिक्के अब तक मिल चुके हैं और अधिक संख्या वाले घिस-पिट चुके हैं।
इस सिक्कों पर लगाये गए प्रतीकों और चिह्नों का पूरा अर्थ होता था जिसे आज अनुमान से ही जाना गया है जबकि बुद्धघोष का कहना है कि "रूपसूत्र" में इसका विवरण मिल जाता था। इस ग्रंथ का अभ्यासी "हेरञ्जक" कहलाता था और वह चित्र-विचित्र सिक्के देखकर निम्न बातें कह सकता था :
1. कोई सिक्का किस गांव, निगम या राजधानी है ?
2. सिक्का किस टकसाल में ढाला गया है ?
3. उसका मूल्य व धातु क्या-क्या है ?
यही नहीं, हेरञ्जक यह भी बता सकता था कि सिक्कों वाला गांव, निगम आदि किस दिशा, पहाड़ी के शिखर या नदी के तट पर मौजूद है। ( Bhudhhistic studies p. 432)
है न रोचक किताब की बात। यह पुस्तक कीमती इसलिये थी कि उसके अभ्यास से सिक्कों की पहचान करते-करते आंखें खोने का भय नहीं रहता था। इसीलिये सर्राफ लोग भी उसका अभ्यास करते थे। क्या यह ग्रंथ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व विद्यालयों में पढ़ाया जाता था ?
मुझे तो मालूम नहीं मगर यह ग्रंथ एक आवश्यकता थी, यह एक प्रमाण की उपज था और इसी आवश्यता ने बाद में मुद्राशास्त्र को जन्म दिया लेकिन क्या हम वह "रूपसूत्र" लौटा सके ? आप इस कुंजी के बारे क्या जानते हैं, जरूर बताइयेगा।
जय-जय।
( रिपोस्ट)
(मित्रों से अधिकाधिक शेयर करने का आग्रह है)
आदिवासियों का श्रृंगार है - कंघी.......!
कंघी से हम सभी परिचित है। बाल संवारने के लिये हम सभी कंघी का उपयोग करते है। प्लास्टिक से बने हुये तरह तरह के कंघे कंघियां बाजारों मे उपलब्ध है और हमारो घरों में भी।
बस्तर के आदिवासियों को कंघी से कुछ ज्यादा ही लगाव देखने को मिलता है। वैसे यह लगाव हर उस व्यक्ति को होता है जो अपने बालों के प्रति अधिक मोह रखता है इस कारण लोग जेब में भी छोटी कंघी रखते है।
बस्तर में महिलायें और पुरूष दोनों ही बांस से बनी कंधी का ही उपयोग करते आ रहे है। आजकल बांस से बनी कंघी उपलब्ध ना होने के कारण प्लास्टिक की कंघी का ही उपयोग करते है।
कंघी केश सज्जा के काम तो आती ही परन्तु बस्तर में महिला एवं पुरूषों दोनों के श्रृंगार में कंघी का स्थान महत्वपूर्ण है। कंघी स्त्री पुरूष दोनों के बालों की शोभा बढ़ाती है। लंबे केश रखने वाली आदिवासी महिलायें अपने बालों में कंघी को हरदम खोंस कर रखती है। बालों के जुड़े में एक दो या कभी कभी तीन छोटी छोटी कंघी खोसी हुई जरूर दिखाई पड़ती है। बांस की कंघियों का स्थान अब प्लास्टिक की कंघी ने ले लिया है। फैशन की हवा अब बस्तर में भी फैल चुकी है जिसके कारण हरदम बालों में कंघी रखने वाली आदिवासी महिलायें अब बिरले ही दिखाई पड़ती है।
आदिवासी युवतियों का कंघी प्रेम तो समझ में आता है परन्तु बस्तरिया युवक भी बालों में दो तीन कंघी जरूर खोसे रखते है। पहले यहां के युवक भी लंबे बाल रखने के शौकिन थे जिसके कारण वे कंघी को हमेशा बालों के जुड़े में खोसे रखते थे। अब स्टायलिश हेयर कट के कारण कंघी बालों के जगह जेब में रहने लग गई है।
बस्तर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कंघी का उपयोग प्रेम निवेदन के लिये भी होता है। कुछ आदिवासी जनजातियों में प्रेम की अभिव्यक्ति हेतु एक नवयुवक एक नवयुवती को बांस से बनी कंघी पेश करता है, जिसे स्वीकार करने पर यह समझा जाता है की उसे युवक का प्रेम निवेदन स्वीकार है।
यहां के विभिन्न जनजातियों में कंघी में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। माड़िया जाति के लोग पनिया, भतरा जाति में कोकोई और बाईसन हार्न माड़िया कंघी को ईसर कहते है।
अब तो लकड़ी या बांस की बनी कंघी देखने को ही नही मिलती है, और तो और आदिवासी युवतियां भी अब प्लास्टिक की कंघी भी बालों में लगाकर रखना पसंद नहीं करती। आदिवासी युवकों ने तो बाल ही छोटे करवा लिये है तो कंघी खोसने की जगह ही नहीं बची, बचे है तो बस ये फोटो।
सुप्रभात... सुबह उठने के बाद मेरा पहला काम कंघी करना ही होता है... 😊
आप हमे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं..!
कंघी से हम सभी परिचित है। बाल संवारने के लिये हम सभी कंघी का उपयोग करते है। प्लास्टिक से बने हुये तरह तरह के कंघे कंघियां बाजारों मे उपलब्ध है और हमारो घरों में भी।
बस्तर के आदिवासियों को कंघी से कुछ ज्यादा ही लगाव देखने को मिलता है। वैसे यह लगाव हर उस व्यक्ति को होता है जो अपने बालों के प्रति अधिक मोह रखता है इस कारण लोग जेब में भी छोटी कंघी रखते है।
बस्तर में महिलायें और पुरूष दोनों ही बांस से बनी कंधी का ही उपयोग करते आ रहे है। आजकल बांस से बनी कंघी उपलब्ध ना होने के कारण प्लास्टिक की कंघी का ही उपयोग करते है।
कंघी केश सज्जा के काम तो आती ही परन्तु बस्तर में महिला एवं पुरूषों दोनों के श्रृंगार में कंघी का स्थान महत्वपूर्ण है। कंघी स्त्री पुरूष दोनों के बालों की शोभा बढ़ाती है। लंबे केश रखने वाली आदिवासी महिलायें अपने बालों में कंघी को हरदम खोंस कर रखती है। बालों के जुड़े में एक दो या कभी कभी तीन छोटी छोटी कंघी खोसी हुई जरूर दिखाई पड़ती है। बांस की कंघियों का स्थान अब प्लास्टिक की कंघी ने ले लिया है। फैशन की हवा अब बस्तर में भी फैल चुकी है जिसके कारण हरदम बालों में कंघी रखने वाली आदिवासी महिलायें अब बिरले ही दिखाई पड़ती है।
आदिवासी युवतियों का कंघी प्रेम तो समझ में आता है परन्तु बस्तरिया युवक भी बालों में दो तीन कंघी जरूर खोसे रखते है। पहले यहां के युवक भी लंबे बाल रखने के शौकिन थे जिसके कारण वे कंघी को हमेशा बालों के जुड़े में खोसे रखते थे। अब स्टायलिश हेयर कट के कारण कंघी बालों के जगह जेब में रहने लग गई है।
बस्तर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कंघी का उपयोग प्रेम निवेदन के लिये भी होता है। कुछ आदिवासी जनजातियों में प्रेम की अभिव्यक्ति हेतु एक नवयुवक एक नवयुवती को बांस से बनी कंघी पेश करता है, जिसे स्वीकार करने पर यह समझा जाता है की उसे युवक का प्रेम निवेदन स्वीकार है।
यहां के विभिन्न जनजातियों में कंघी में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। माड़िया जाति के लोग पनिया, भतरा जाति में कोकोई और बाईसन हार्न माड़िया कंघी को ईसर कहते है।
अब तो लकड़ी या बांस की बनी कंघी देखने को ही नही मिलती है, और तो और आदिवासी युवतियां भी अब प्लास्टिक की कंघी भी बालों में लगाकर रखना पसंद नहीं करती। आदिवासी युवकों ने तो बाल ही छोटे करवा लिये है तो कंघी खोसने की जगह ही नहीं बची, बचे है तो बस ये फोटो।
सुप्रभात... सुबह उठने के बाद मेरा पहला काम कंघी करना ही होता है... 😊
आप हमे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं..!
#पर्दाप्रथा --( भाग -1)
---------------------------
प्राचीन भारत में 100 ईसा पूर्व तक पर्दा अज्ञात था।
वैदिक से महाकाव्य कालीन जीवन तक -- लड़कों के साथ - साथ लड़कियाँ भी प्रायः शिक्षित की जाती थीं..इसके प्रमाण उपलब्ध है। उत्तररामचरित में आत्रेयी के उदाहरण से स्पष्ट है जो राम के पुत्रों लव और कुश के साथ साथ वाल्मीकि के सानिध्य में पढ़ रही थी।
प्रेम - विवाह विरल रूप से नहीं घटित होते थे , और ( युवक / युवतियाँ ) उनके प्रेम को जीतने के लिये उनकी / उनके प्रेमिकाओं / प्रेमियों के पास जा सकते थे , और दोनों प्रदर्शनों तथा क्रीडाओं को देखने के लिये प्रायः एक साथ जाया करते थे ।
यदि समाज में कुमारियों के द्वारा पर्दा - प्रथा का पालन किया गया होता , तो यह सब सम्भव नहीं हो गया होता ।
न विवाह के बाद में सामान्य स्थिति बदलती थी ।
ऋग्वेद का " विवाह - सूक्त"-
सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत।
सौभाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं वि परेतन।।
और
वशिनी त्वं विदथमावदासि।
यानि --यह सूक्त --विवाह के धार्मिक कृत्य के अन्त में समस्त एकत्रित अतिथियों को वधू को दिखायी जाने की अपेक्षा रखता है । ' यह और आगे आशा की जाती थी कि वधू उसकी वृद्धावस्था तक सार्वजनिक सभाओं में शान्ति के साथ बोलने के लिये समर्थ होनी चाहिये ।
वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक और सार्वजनिक सभाओं में उपस्थिति एक सामान्य विशेषता थी ।
अथर्ववेद की इस सूक्ती से --" जुष्टा नरेषु समनेषु वल्गु " से ज्ञात होता है कि नारी -- समाज के लिए बिलकुल अभिनन्दनीय थी ।
जब कभी कुछ भी मनोहर अथवा ललित का वर्णन किया जाना है , वैदिक कवि ( ऋषि ) एक उत्सव के लिये बाहर जाती हुई प्रफुल्लतापूर्वक वेशभूषा से सज्जित महिला के विषय में तुलना के एक मानक पात्र के रूप में प्रायः सोचते हैं ( ऋग्वेद )
निरुक्त ( लगभग 500 ई.पू. ) से हम ज्ञात करते हैं कि महिलाएँ उत्तराधिकार के उनके दावों को स्थापित करने के लिये विधि - न्यायालयों की ओर बाहर जाया करती थीं ...
उनकी उपस्थिति के लिये कोई पर्दाव्यवस्था की जाने का वहाँ कोई भी सन्दर्भ नहीं है ।
न ऋग्वेद--पर्दा - प्रथा का कोई सन्दर्भ अन्तर्विष्ट करता है ।
मिम्यक्ष यषु सुधिता घृताची हिरण्यनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः ।
गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सभावती विदथ्येव सं वाक् ।
अर्थात -- अब घृतपात्र में डुबाई जाती हुई और तत्पश्चात् बाहर निकाली जाती हुई तथा उसकी अन्तर्वस्तुओं ( आहुतियों ) को याज्ञिक अग्नि में ऊँडेलने के लिये आगे लायी जाती हुई दर्वी ( कलछी ) की अब उसके घर के एकान्त स्थान में रहती हुई , और तत्पश्चात् एक बैठक ( उपवेशन ) में उपस्थित होने के लिये जनसाधारण में बाहर आती हुई एक महिला से इस मन्त्र में तुलना की जाती है ।
-----
Pappusingh prajapat
---------------------------
प्राचीन भारत में 100 ईसा पूर्व तक पर्दा अज्ञात था।
वैदिक से महाकाव्य कालीन जीवन तक -- लड़कों के साथ - साथ लड़कियाँ भी प्रायः शिक्षित की जाती थीं..इसके प्रमाण उपलब्ध है। उत्तररामचरित में आत्रेयी के उदाहरण से स्पष्ट है जो राम के पुत्रों लव और कुश के साथ साथ वाल्मीकि के सानिध्य में पढ़ रही थी।
प्रेम - विवाह विरल रूप से नहीं घटित होते थे , और ( युवक / युवतियाँ ) उनके प्रेम को जीतने के लिये उनकी / उनके प्रेमिकाओं / प्रेमियों के पास जा सकते थे , और दोनों प्रदर्शनों तथा क्रीडाओं को देखने के लिये प्रायः एक साथ जाया करते थे ।
यदि समाज में कुमारियों के द्वारा पर्दा - प्रथा का पालन किया गया होता , तो यह सब सम्भव नहीं हो गया होता ।
न विवाह के बाद में सामान्य स्थिति बदलती थी ।
ऋग्वेद का " विवाह - सूक्त"-
सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत।
सौभाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं वि परेतन।।
और
वशिनी त्वं विदथमावदासि।
यानि --यह सूक्त --विवाह के धार्मिक कृत्य के अन्त में समस्त एकत्रित अतिथियों को वधू को दिखायी जाने की अपेक्षा रखता है । ' यह और आगे आशा की जाती थी कि वधू उसकी वृद्धावस्था तक सार्वजनिक सभाओं में शान्ति के साथ बोलने के लिये समर्थ होनी चाहिये ।
वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक और सार्वजनिक सभाओं में उपस्थिति एक सामान्य विशेषता थी ।
अथर्ववेद की इस सूक्ती से --" जुष्टा नरेषु समनेषु वल्गु " से ज्ञात होता है कि नारी -- समाज के लिए बिलकुल अभिनन्दनीय थी ।
जब कभी कुछ भी मनोहर अथवा ललित का वर्णन किया जाना है , वैदिक कवि ( ऋषि ) एक उत्सव के लिये बाहर जाती हुई प्रफुल्लतापूर्वक वेशभूषा से सज्जित महिला के विषय में तुलना के एक मानक पात्र के रूप में प्रायः सोचते हैं ( ऋग्वेद )
निरुक्त ( लगभग 500 ई.पू. ) से हम ज्ञात करते हैं कि महिलाएँ उत्तराधिकार के उनके दावों को स्थापित करने के लिये विधि - न्यायालयों की ओर बाहर जाया करती थीं ...
उनकी उपस्थिति के लिये कोई पर्दाव्यवस्था की जाने का वहाँ कोई भी सन्दर्भ नहीं है ।
न ऋग्वेद--पर्दा - प्रथा का कोई सन्दर्भ अन्तर्विष्ट करता है ।
मिम्यक्ष यषु सुधिता घृताची हिरण्यनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः ।
गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सभावती विदथ्येव सं वाक् ।
अर्थात -- अब घृतपात्र में डुबाई जाती हुई और तत्पश्चात् बाहर निकाली जाती हुई तथा उसकी अन्तर्वस्तुओं ( आहुतियों ) को याज्ञिक अग्नि में ऊँडेलने के लिये आगे लायी जाती हुई दर्वी ( कलछी ) की अब उसके घर के एकान्त स्थान में रहती हुई , और तत्पश्चात् एक बैठक ( उपवेशन ) में उपस्थित होने के लिये जनसाधारण में बाहर आती हुई एक महिला से इस मन्त्र में तुलना की जाती है ।
-----
Pappusingh prajapat
बस्तर के मृतक स्तंभ....!
बस्तर के जनजातियों मे पाषाण युगीन प्रागैतिहासिक मृतक संस्कारों की प्रथा वर्तमान समय मे भी प्रचलित है। मुरिया, राजा मुरिया, डंडामि माड़िया तथा अबूझ माड़िया जनजातियों मे मृतक संस्कारों की यह पाषाण युगीन परंपरा विद्यमान है। इन सभी जन- जातियों मे मृतक के संस्कार मे स्मृति स्वरूप एक शिला शव स्थान मे खड़ी की जाती है। इन पाषाण शिलाओं को उरसगट्टा, मेनहिर, उर्सकाल, कोटोकल या सामान्य भाषा मे मृतक स्तंभ कहा जाता है कही कही पर शिला खड़ी न कर शव स्थानों पर ही पत्थरों को सहेज कर जमा कर दिया जाता है जो धीरे-धीरे पत्थरों का एक ढेर बन जाता है जिसे स्थानीय लोग मठ कहते है।
उरसकाल जिसका गोंडी बोली मे अर्थ उरसाना- दफनाना, और कल- पत्थर होता है मृतक के स्मृति मे मृतक स्तंभ की मृतक स्तंभ की स्थापना की जाती है। बस्तर के संभाग के प्रमुख जिले- दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागाव के क्षेत्रों मे इन मृतक स्तंभों की श्रृंखला मिलती है। दंतेवाड़ा के गामावाड़ा मे एक बड़ी श्रृंखला मे पाषाण युग के मृतक स्तंभ स्थापित है... राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 पर दंतेवाड़ा से जगदलपुर मार्ग पर स्थित डिलमिलि, मावली भाटा ग्राम मे मुख्य मार्ग के दोनों ओर इनकी श्रृंखला अवस्थित है... !
यह शिला स्लेटी लाल रंग की होती है.. इन मृतक स्तंभों का आकर्षण इनकी चित्रकारी है.. जिन पर आधुनिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। नृत्य, समारोह, पशु- पक्षियों के साथ साथ लंदा (चावल की शराब) पीते स्त्री- पुरुष की का चित्र, हवाई जहाज, कार आदि का चित्र जीवन की लौकिकता को प्रदर्शित करता है। गीदम के जावंगा और बस्तर के डीलमिलि मे काष्ठ के मृतक स्तंभ भी है...!
मेनहीर गाड़ने की परंपरा मुरिया एवम मारिया मृतक संस्कार की विशिष्ट परम्परा है। जब इन जनजातियों मे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ढोल का एक विशेष नाद बजाया जाता है मुख्यत दामाँद द्वारा। जिससे सभी को सूचना मिल जाती है कि इस घर मे दुःख हो गया है। इन जनजातियों मे मृतक को दफनाने की प्रथा है। इस प्रक्रिया के बाद ग्राम के ही कुछ व्यक्तियों को ही जो पत्थर को काटने का कार्य करते है उनसे पहाड़ से शिला काटने का आग्रह किया जाता है। शिला को काटने के बाद उसे खींच कर लाने की परंपरा है जो भांजा पूरी करता है वह तेजी से ढोल को पीटता हैं और अपने गंतव्य की चल पड़ता है और शेष लोग पत्थर को खीच कर लाते है इस समय ढोल की नाद पर कुछ लोग नृत्य भी करते है।
शिला को उस स्थान पर लाया जाता जहाँ पहले से गड्ढा खोदकर रख दिया गया हो, आगे की प्रक्रिया मे ग्राम का गयता परिवार जनो को अपने देव और पेन पुरखा को याद करने के लिए कहता है। मृतक चुकि अलग लोक मे चला गया है तो उसे किसी भी प्रकार की समस्या न हो इस लिए परिवार जन गड्ढे मे थोड़ा अनाज, सिक्के भी डालते है यह एक नेन्ग है। इसके बाद शिला को गड्ढे मे स्थापित किया जाता हैं तथा इसके सामने छोटा सा पत्थर और रखा जाता है जिस समय समय पर देव कार्य किया जाता है मुख्य रूप से जनजातियों का की मान्यता है मृत व्यक्ति अब उनकी पेन शक्ति या अलौकिक शक्ति मे विलीन हो गया है। जिसे देव कार्य एवं आयोजनों पर स्मरण कर बलि भी दी जाती है।
मृतक स्तंभ की इस परंपरा को जनजातिय समाज से ही संपूर्ण वैश्विक समाज ने आत्मसात किया हैं।
लेख एवम चित्र
आशीष कुमेटी
बस्तर के जनजातियों मे पाषाण युगीन प्रागैतिहासिक मृतक संस्कारों की प्रथा वर्तमान समय मे भी प्रचलित है। मुरिया, राजा मुरिया, डंडामि माड़िया तथा अबूझ माड़िया जनजातियों मे मृतक संस्कारों की यह पाषाण युगीन परंपरा विद्यमान है। इन सभी जन- जातियों मे मृतक के संस्कार मे स्मृति स्वरूप एक शिला शव स्थान मे खड़ी की जाती है। इन पाषाण शिलाओं को उरसगट्टा, मेनहिर, उर्सकाल, कोटोकल या सामान्य भाषा मे मृतक स्तंभ कहा जाता है कही कही पर शिला खड़ी न कर शव स्थानों पर ही पत्थरों को सहेज कर जमा कर दिया जाता है जो धीरे-धीरे पत्थरों का एक ढेर बन जाता है जिसे स्थानीय लोग मठ कहते है।
उरसकाल जिसका गोंडी बोली मे अर्थ उरसाना- दफनाना, और कल- पत्थर होता है मृतक के स्मृति मे मृतक स्तंभ की मृतक स्तंभ की स्थापना की जाती है। बस्तर के संभाग के प्रमुख जिले- दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागाव के क्षेत्रों मे इन मृतक स्तंभों की श्रृंखला मिलती है। दंतेवाड़ा के गामावाड़ा मे एक बड़ी श्रृंखला मे पाषाण युग के मृतक स्तंभ स्थापित है... राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 पर दंतेवाड़ा से जगदलपुर मार्ग पर स्थित डिलमिलि, मावली भाटा ग्राम मे मुख्य मार्ग के दोनों ओर इनकी श्रृंखला अवस्थित है... !
यह शिला स्लेटी लाल रंग की होती है.. इन मृतक स्तंभों का आकर्षण इनकी चित्रकारी है.. जिन पर आधुनिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। नृत्य, समारोह, पशु- पक्षियों के साथ साथ लंदा (चावल की शराब) पीते स्त्री- पुरुष की का चित्र, हवाई जहाज, कार आदि का चित्र जीवन की लौकिकता को प्रदर्शित करता है। गीदम के जावंगा और बस्तर के डीलमिलि मे काष्ठ के मृतक स्तंभ भी है...!
मेनहीर गाड़ने की परंपरा मुरिया एवम मारिया मृतक संस्कार की विशिष्ट परम्परा है। जब इन जनजातियों मे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ढोल का एक विशेष नाद बजाया जाता है मुख्यत दामाँद द्वारा। जिससे सभी को सूचना मिल जाती है कि इस घर मे दुःख हो गया है। इन जनजातियों मे मृतक को दफनाने की प्रथा है। इस प्रक्रिया के बाद ग्राम के ही कुछ व्यक्तियों को ही जो पत्थर को काटने का कार्य करते है उनसे पहाड़ से शिला काटने का आग्रह किया जाता है। शिला को काटने के बाद उसे खींच कर लाने की परंपरा है जो भांजा पूरी करता है वह तेजी से ढोल को पीटता हैं और अपने गंतव्य की चल पड़ता है और शेष लोग पत्थर को खीच कर लाते है इस समय ढोल की नाद पर कुछ लोग नृत्य भी करते है।
शिला को उस स्थान पर लाया जाता जहाँ पहले से गड्ढा खोदकर रख दिया गया हो, आगे की प्रक्रिया मे ग्राम का गयता परिवार जनो को अपने देव और पेन पुरखा को याद करने के लिए कहता है। मृतक चुकि अलग लोक मे चला गया है तो उसे किसी भी प्रकार की समस्या न हो इस लिए परिवार जन गड्ढे मे थोड़ा अनाज, सिक्के भी डालते है यह एक नेन्ग है। इसके बाद शिला को गड्ढे मे स्थापित किया जाता हैं तथा इसके सामने छोटा सा पत्थर और रखा जाता है जिस समय समय पर देव कार्य किया जाता है मुख्य रूप से जनजातियों का की मान्यता है मृत व्यक्ति अब उनकी पेन शक्ति या अलौकिक शक्ति मे विलीन हो गया है। जिसे देव कार्य एवं आयोजनों पर स्मरण कर बलि भी दी जाती है।
मृतक स्तंभ की इस परंपरा को जनजातिय समाज से ही संपूर्ण वैश्विक समाज ने आत्मसात किया हैं।
लेख एवम चित्र
आशीष कुमेटी