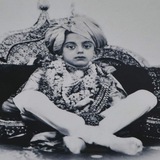ा दी थी, उन्होंने कहा था कि राजाओं के बच्चे भारतीय भाषा एवं संस्कृति से दूर अंग्रेजों की बुराईयों को अपनाने लगते है, जबकि इंग्लैंड में राजा के बच्चे आम आदमी की तरह जीवन जीते हैं।
हमारे देश में अंग्रेजों की अच्छाई को राजाओं द्वारा नहीं अपनाया जाता जबकि अंग्रेजों की बुराइयों जैसे नशा करना एवं जुआ खेलना को सहज अपना लेते है। गाँधी ने इनसे बचने की सीख दी थी, छत्तीसगढ़ का दौरा समाप्त कर गाँधी बालाघाट होते हुए इटारसी चले गये थे।
छत्तीसगढ़ में गांधी दो बार आये, पहली बार मोहनदास बनकर दूसरी बार महात्मा बनकर, और इन दोनो ही यात्राओं के दौरान गांधी ने छत्तीसगढ़ के समाज और प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया। पं. रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल, घनश्याम सिंह गुप्त, ई. राघेवेन्द्र राव, बाबु छोटेलाल श्रीवास्तव जैसे हजारों नेता गाँधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आजीवन देश की सेवा में लग गये।
तत्कालीन मध्य एवं बराड़ प्रांत का सर्वाधिक राजनैतिक दृष्टि से जागरूक क्षेत्र छत्तीसगढ़ बन कर उभरा हुआ था। गाँधी के प्रभाव से युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में राजनीति मे आई जिसने 1940-42 के स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया। यही कारण था कि जब मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना हुई उस समय नये राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए नेता थे।
महात्मा गाँधी का महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्र में छूआछूत जैसी समस्या के समाधान मे देखने को मिलता है। हालांकि छत्तीसगढ़ मे अछूत उद्धार कार्यक्रम महात्मा गाँधी के प्रयासों से पूर्व पं. सुन्दरलाल शर्मा ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरूआत कर दी थी, इसके बाद गाँधी का भी प्रभाव था
छत्तीसगढ़ मे भेदभाव की भावना अपेक्षाकृत न्यून रही। गाँधी के छत्तीसगढ़ पर महत्वपूर्ण प्रभाव बुनकर सहकारी आंदोलनों मे भी देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई क्षेत्र हो जहां हथकरघा से बुने सूती वस्त्रों का निर्माण नहीं होता है। बाकायदा सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे प्रदेश एवं देश भर मे सूती और सिल्क के वस्त्रों का व्यापार भी होता है।
छत्तीसगढ़ की जीवनशैली में सादगी एवं सरलता सत्य एवं शांति प्रियता भी गाँधी के मत आधारित है। गाँधी वैसे भी भारतीय सनातन सिद्धांत के अग्रदूत थे जो समाज को सदैव प्रगतिशील मार्ग दिखाते हैं। यह विचार वैदिक साहित्यों से गाँधी तक अविरल प्रवाहित है और समय के साथ या और भी देश और दुनिया में प्रांसगिक बने रहेंगें।
आलेख
शशांक शर्मा रायपुर
वरिष्ठ लेखक एवं चितंक
हमारे देश में अंग्रेजों की अच्छाई को राजाओं द्वारा नहीं अपनाया जाता जबकि अंग्रेजों की बुराइयों जैसे नशा करना एवं जुआ खेलना को सहज अपना लेते है। गाँधी ने इनसे बचने की सीख दी थी, छत्तीसगढ़ का दौरा समाप्त कर गाँधी बालाघाट होते हुए इटारसी चले गये थे।
छत्तीसगढ़ में गांधी दो बार आये, पहली बार मोहनदास बनकर दूसरी बार महात्मा बनकर, और इन दोनो ही यात्राओं के दौरान गांधी ने छत्तीसगढ़ के समाज और प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया। पं. रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल, घनश्याम सिंह गुप्त, ई. राघेवेन्द्र राव, बाबु छोटेलाल श्रीवास्तव जैसे हजारों नेता गाँधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आजीवन देश की सेवा में लग गये।
तत्कालीन मध्य एवं बराड़ प्रांत का सर्वाधिक राजनैतिक दृष्टि से जागरूक क्षेत्र छत्तीसगढ़ बन कर उभरा हुआ था। गाँधी के प्रभाव से युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में राजनीति मे आई जिसने 1940-42 के स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया। यही कारण था कि जब मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना हुई उस समय नये राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए नेता थे।
महात्मा गाँधी का महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्र में छूआछूत जैसी समस्या के समाधान मे देखने को मिलता है। हालांकि छत्तीसगढ़ मे अछूत उद्धार कार्यक्रम महात्मा गाँधी के प्रयासों से पूर्व पं. सुन्दरलाल शर्मा ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरूआत कर दी थी, इसके बाद गाँधी का भी प्रभाव था
छत्तीसगढ़ मे भेदभाव की भावना अपेक्षाकृत न्यून रही। गाँधी के छत्तीसगढ़ पर महत्वपूर्ण प्रभाव बुनकर सहकारी आंदोलनों मे भी देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई क्षेत्र हो जहां हथकरघा से बुने सूती वस्त्रों का निर्माण नहीं होता है। बाकायदा सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे प्रदेश एवं देश भर मे सूती और सिल्क के वस्त्रों का व्यापार भी होता है।
छत्तीसगढ़ की जीवनशैली में सादगी एवं सरलता सत्य एवं शांति प्रियता भी गाँधी के मत आधारित है। गाँधी वैसे भी भारतीय सनातन सिद्धांत के अग्रदूत थे जो समाज को सदैव प्रगतिशील मार्ग दिखाते हैं। यह विचार वैदिक साहित्यों से गाँधी तक अविरल प्रवाहित है और समय के साथ या और भी देश और दुनिया में प्रांसगिक बने रहेंगें।
आलेख
शशांक शर्मा रायपुर
वरिष्ठ लेखक एवं चितंक
अनूठे अतीत का साक्षी है सुकमा का चिटमटिन माता मंदिर
[नवरात्रि पर विशेष आलेख श्रंखला - चौथी कड़ी]
--------------------------------
सुकमा का इतिहास कई मायनों में रोचक है। उस क्षेत्र की प्रधान आराध्य देवी रामारामिन अथवा चिटमटिन की चर्चा से पूर्व संक्षेप में यहाँ का अतीत जानना आवश्यक है। सुकमा को जिले का दर्जा आज मिला है किंतु राजतंत्र के दौर में यह एक महत्वपूर्ण जमींदारी हुआ करती थी। इस जमींदारी के अंतर्गत लगभग 650 वर्गमील का क्षेत्र आता था जिसमें 128 गाँव सम्मिलित थे। यह गौर करने वाला तथ्य है कि बस्तर रियासत के अंतर्गत केवल सुकमा जमींदारी ही ऐसी थी जिसके जमींदार क्षत्रिय थे जबकि शेष जमींदारियों पर गोंड़ शासक थे। यहाँ के जमीदारों के सम्बन्ध में बड़ा ही अविश्वसनीय वृतांत मिलता है जिसके अनुसार पाँच सौ वर्ष पहले जब रंगाराज यहाँ शासक थे उनके चार पुत्र - रामराज, मोतीराज, सुब्बाराज तथा रामराज, राज्य को ले कर विवाद कर बैठे। विवश हो कर सुकमा जमीन्दारी के चार हिस्से किये गये जो थे सुकमा, भीजी, राकापल्ली तथा चिन्तलनार। कहते हैं राजा ने इसके बाद अपने पुत्रों को शाप दिया कि अब सुकमा की गद्दी के लिये एक ही पुत्र बचेगा साथ ही आनेवाली पीढ़ियों के केवल दो ही नाम रखे जायेंगे रामराज और रंगाराज। यदि तथ्यों को परखा जाये तो राजतंत्र की समाप्ति तक सुकमा के जमीनदारों की लगभग 11 पीढ़ी के नाम क्रमिकता में रामराज और रंगाराज ही रखे गये। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बस्तर पर चालुक्य राजाओं के अधिकार के पश्चात सुकमा के जमींदारों ने वहाँ के राजाओं से हमेशा वैवाहिक सम्बन्ध बना कर रखे इस कारण इस जमींदारी का न केवल महत्व बढ़ा अपितु यह शक्तिशाली भी हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में स्थित सुकमा जिले की सीमा उड़ीसा और तेलंगाना के साथ लगती है। सुकमा क्षेत्र में मुरिया तथा परजा को मुख्य निवासी कहा जाता है साथ ही यह क्षेत्र दोरला आदिवासियों का प्रमुख गढ़ है।
अब बात सुकमा की प्रधान देवी रामारामिन की कर लेते हैं। मध्य बस्तर और उत्तर बस्तर से पुरातात्विक महत्व के अनेक मंदिर व प्रतिमायें चर्चित हुई हैं एवं पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पहुँचने में लोगों की बहुत रुचि भी है। दक्षिण बस्तर पर कम ही चर्चायें हुईं हैं। बारसूर एवं दंतेवाड़ा से आगे कम पर्यटक बढ़ते हैं। इसका पहला कारण तो वह सड़क व्यवस्था है जो दंतेवाड़ा से आगे सुकमा-कोण्टा को जोड़ती है। यही स्थिति दंतेवाड़ा से भोपालपट्टनम को जोड़ने वाली सड़क की भी है। नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण आये दिन सड़क खोद दी जाती है और आवागमन बाधित हो जाता है। दूसरा कारण है कि इन क्षेत्रों पर बहुत कम शोधकर्ताओं ने कलम चलाई है। रियासतकाल में सुकमा जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण जमींदारी वृहद बस्तर जिले की छाया में निश्चित ही उपेक्षित महसूस कर रही थी। जिला बन जाने के पश्चात से सुकमा की रौनक कुछ हद तक लौटी है।सुकमा में रियासतकालीन जमींदार भवन दर्शनीय है। आसपास बिखरी हुई बहुत सी पुरातात्विक महत्व की प्रतिमायें हैं जो पेड़ के नीचे, किसी झुरमुट में, नदी के किनारे या सड्क़ के किनारे धूल, मिट्टी, पानी को झेलती हुई भी सदियों से अवस्थित हैं। सुकमा नगर के बाहरी छोर पर स्थित रामारामिन माता का मंदिर जिसे चिटमटिन अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है तथा पूरे नगर की आस्था के केन्द्र में है। मंदिर के सामने की ओर अनेक चबूतरे निर्मित किये गये हैं जो फरवरी माह में यहाँ लगने वाले मेले के दौरान उपयोग में लाये जाते हैं। ऐतिहासिक समय से ही राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के कारण इस मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली में दर्शनीय निर्माण करवाया गया है।
मंदिर से लग कर ही एक पहाड़ी है जिसपर चढ़ने के पश्चात आसपास का नज़ारा बहुत ही रमणीक दिखाई पड़ता है। पहाड़ी के उपर प्राचीन मंदिर के कुछ अवशेष हैं। उसी से जोड़ कर अनेक किंवदंतियाँ भी इस अंचल में प्रसारित हैं। एक स्थानीय ने बताया कि कभी माता चिटमटीन का मंदिर उपर पहाड़ी पर हुआ करता था। कहते हैं कि पुजारी की देरी से नाराज देवी ने पूजा का लोटा और थाल फेंक दिया। एक प्रस्तर पर उकेरी गयी थाल जैसी आकृति को फेंकी गयी थाली का प्रतीक कहा जाता है जबकि जहाँ लोटा गिरा उस स्थल पर वर्तमान में अवस्थित मंदिर का निर्माण किया गया, बताया जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने के पश्चात यह महसूस होता है कि इस स्थल का उपयोग निश्चित तौर पर प्राचीन शिल्पकार अथवा कारीगर किया करते होंगे। पत्थरों में स्थान स्थान पर गोलाकार छिद्र हैं। पहाड़ी के बिलकुल शीर्ष पर एक कुण्ड नुमा पानी का सोता भी है। चूंकि गर्मियों में भी इस कुण्ड का जल नहीं सूखता अत: पवित्र माना जाता है, इससे स्थान की धार्मिक महत्ता बढ़ गयी है। वस्तुत: रहस्य और इतिहास की कई परतों के पीछे छिपा है सुकमा का चिटमटिन माता मंदिर।
- राजीव रंजन प्रसाद
===========
[नवरात्रि पर विशेष आलेख श्रंखला - चौथी कड़ी]
--------------------------------
सुकमा का इतिहास कई मायनों में रोचक है। उस क्षेत्र की प्रधान आराध्य देवी रामारामिन अथवा चिटमटिन की चर्चा से पूर्व संक्षेप में यहाँ का अतीत जानना आवश्यक है। सुकमा को जिले का दर्जा आज मिला है किंतु राजतंत्र के दौर में यह एक महत्वपूर्ण जमींदारी हुआ करती थी। इस जमींदारी के अंतर्गत लगभग 650 वर्गमील का क्षेत्र आता था जिसमें 128 गाँव सम्मिलित थे। यह गौर करने वाला तथ्य है कि बस्तर रियासत के अंतर्गत केवल सुकमा जमींदारी ही ऐसी थी जिसके जमींदार क्षत्रिय थे जबकि शेष जमींदारियों पर गोंड़ शासक थे। यहाँ के जमीदारों के सम्बन्ध में बड़ा ही अविश्वसनीय वृतांत मिलता है जिसके अनुसार पाँच सौ वर्ष पहले जब रंगाराज यहाँ शासक थे उनके चार पुत्र - रामराज, मोतीराज, सुब्बाराज तथा रामराज, राज्य को ले कर विवाद कर बैठे। विवश हो कर सुकमा जमीन्दारी के चार हिस्से किये गये जो थे सुकमा, भीजी, राकापल्ली तथा चिन्तलनार। कहते हैं राजा ने इसके बाद अपने पुत्रों को शाप दिया कि अब सुकमा की गद्दी के लिये एक ही पुत्र बचेगा साथ ही आनेवाली पीढ़ियों के केवल दो ही नाम रखे जायेंगे रामराज और रंगाराज। यदि तथ्यों को परखा जाये तो राजतंत्र की समाप्ति तक सुकमा के जमीनदारों की लगभग 11 पीढ़ी के नाम क्रमिकता में रामराज और रंगाराज ही रखे गये। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बस्तर पर चालुक्य राजाओं के अधिकार के पश्चात सुकमा के जमींदारों ने वहाँ के राजाओं से हमेशा वैवाहिक सम्बन्ध बना कर रखे इस कारण इस जमींदारी का न केवल महत्व बढ़ा अपितु यह शक्तिशाली भी हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में स्थित सुकमा जिले की सीमा उड़ीसा और तेलंगाना के साथ लगती है। सुकमा क्षेत्र में मुरिया तथा परजा को मुख्य निवासी कहा जाता है साथ ही यह क्षेत्र दोरला आदिवासियों का प्रमुख गढ़ है।
अब बात सुकमा की प्रधान देवी रामारामिन की कर लेते हैं। मध्य बस्तर और उत्तर बस्तर से पुरातात्विक महत्व के अनेक मंदिर व प्रतिमायें चर्चित हुई हैं एवं पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पहुँचने में लोगों की बहुत रुचि भी है। दक्षिण बस्तर पर कम ही चर्चायें हुईं हैं। बारसूर एवं दंतेवाड़ा से आगे कम पर्यटक बढ़ते हैं। इसका पहला कारण तो वह सड़क व्यवस्था है जो दंतेवाड़ा से आगे सुकमा-कोण्टा को जोड़ती है। यही स्थिति दंतेवाड़ा से भोपालपट्टनम को जोड़ने वाली सड़क की भी है। नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण आये दिन सड़क खोद दी जाती है और आवागमन बाधित हो जाता है। दूसरा कारण है कि इन क्षेत्रों पर बहुत कम शोधकर्ताओं ने कलम चलाई है। रियासतकाल में सुकमा जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण जमींदारी वृहद बस्तर जिले की छाया में निश्चित ही उपेक्षित महसूस कर रही थी। जिला बन जाने के पश्चात से सुकमा की रौनक कुछ हद तक लौटी है।सुकमा में रियासतकालीन जमींदार भवन दर्शनीय है। आसपास बिखरी हुई बहुत सी पुरातात्विक महत्व की प्रतिमायें हैं जो पेड़ के नीचे, किसी झुरमुट में, नदी के किनारे या सड्क़ के किनारे धूल, मिट्टी, पानी को झेलती हुई भी सदियों से अवस्थित हैं। सुकमा नगर के बाहरी छोर पर स्थित रामारामिन माता का मंदिर जिसे चिटमटिन अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है तथा पूरे नगर की आस्था के केन्द्र में है। मंदिर के सामने की ओर अनेक चबूतरे निर्मित किये गये हैं जो फरवरी माह में यहाँ लगने वाले मेले के दौरान उपयोग में लाये जाते हैं। ऐतिहासिक समय से ही राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के कारण इस मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली में दर्शनीय निर्माण करवाया गया है।
मंदिर से लग कर ही एक पहाड़ी है जिसपर चढ़ने के पश्चात आसपास का नज़ारा बहुत ही रमणीक दिखाई पड़ता है। पहाड़ी के उपर प्राचीन मंदिर के कुछ अवशेष हैं। उसी से जोड़ कर अनेक किंवदंतियाँ भी इस अंचल में प्रसारित हैं। एक स्थानीय ने बताया कि कभी माता चिटमटीन का मंदिर उपर पहाड़ी पर हुआ करता था। कहते हैं कि पुजारी की देरी से नाराज देवी ने पूजा का लोटा और थाल फेंक दिया। एक प्रस्तर पर उकेरी गयी थाल जैसी आकृति को फेंकी गयी थाली का प्रतीक कहा जाता है जबकि जहाँ लोटा गिरा उस स्थल पर वर्तमान में अवस्थित मंदिर का निर्माण किया गया, बताया जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने के पश्चात यह महसूस होता है कि इस स्थल का उपयोग निश्चित तौर पर प्राचीन शिल्पकार अथवा कारीगर किया करते होंगे। पत्थरों में स्थान स्थान पर गोलाकार छिद्र हैं। पहाड़ी के बिलकुल शीर्ष पर एक कुण्ड नुमा पानी का सोता भी है। चूंकि गर्मियों में भी इस कुण्ड का जल नहीं सूखता अत: पवित्र माना जाता है, इससे स्थान की धार्मिक महत्ता बढ़ गयी है। वस्तुत: रहस्य और इतिहास की कई परतों के पीछे छिपा है सुकमा का चिटमटिन माता मंदिर।
- राजीव रंजन प्रसाद
===========
क्या भैंसादोंद डोंगरी में हुआ था महिषासुर वध?
[नवरात्रि पर विशेष आलेख श्रंखला, छठवीं कड़ी]
----------------------------------
महिषासुर के वध स्थल होने का दावा देश के अनेक स्थानों से किया जाता है, बस्तर का बडे डोंगर क्षेत्र भी उनमें से एक है। बस्तर की मान्यता पर विवेचना से पहले इसी कथन से जुडे कुछ प्रचलित स्थलों को जान लेते हैं। दक्षिण भारत का भव्य एतिहासिक शहर है मैसूर। मैसूर शब्द पर ध्यान दीजिये क्योंकि प्रचलित मान्यता है कि एक समय में मैसूर ही महिषासुर की राजधानी ‘महिसुर’ हुआ करती थी; तर्कपूर्ण लगता है कि महिसुर बदल कर मैसूर हो गया हो। मैसूर के निकट की चामुण्डा पर्वत की अवस्थिति है जहाँ यह माना जाता है कि महिषासुर का वध भी यहीं हुआ था। इसी तरह पूर्वी भारत अर्थात हिमांचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी शक्तिपीठ अवस्थित है। पुराणों के अनुसार देवी सती के नैन गिरने के कारण यह शक्तिपीठ स्थापित हुआ किंतु महिषासुर की कथा भी इसी स्थल से जुडी हुई मानी जाती है तथा उसका वध-स्थल भी यहीं पर माना जाता है। कहानियाँ और भी हैं; झारखण्ड के चतरा जिले का भी यह दावा है कि महिषासुर का वध वहीं हुआ। इसके तर्क में तमासीन जलप्रपात के निकट क्षेत्रों में प्रचलित कथा है कि नवरात्र के समय आज भी यहाँ तलवारों की खनक सुनाई देती है तथा यत्र-तत्र सिंदूर बिखरा हुआ देखा जा सकता है।
इन सभी कहानियों से अधिक प्रामाणिक मुझे वह संदर्भ लगता है जो बस्तर की मान्यताओं में अवस्थित है। बस्तर के जिस क्षेत्र का संदर्भ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह हमेशा से ही जंगली भैंसो के लिये विख्यात रहा है; पुनश्च भैंस अर्थात महिष। अपने विशाल स्वरूप और बलिष्ठ काठी के कारण बस्तर के महिष को कभी दैत्याकार लिखा गया तो कभी उसका विवरण भयावहतम शब्दों में प्राचीन पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया है। बस्तर के इन महिषों/जंगली भैंसों पर गल्सफर्ड की डायरी (1860) से लिया गया यह एक विवरण देखें – “इसकी एक सींग साढे अठहत्तर इंच लम्बी होती है। यदि हम मस्तक की खोपड़ी एक फुट चौड़ी माने तो यह सिर से पैर तक चौदह फुट ऊँचा होता है”। यदि इस कहानी का बस्तर से उद्गम माना जाये तो यहाँ के महिष पालतू नहीं थे तथा उनका शिकार किया जाता रहा है। वस्तुत: महिषासुर के वध से जुडी कहानी बस्तर के बड़े डोंगर क्षेत्र से मानी जाती है।
बडे डोंगर में मेरी अभिरुचि पुरातात्विक महत्व के अनेक कारणों से तो थी ही किंतु मैं उस महिषाद्वन्द्व पहाड़ को विशेष रूप से देखना चाहता था जिसे स्थानीय भैंसादोंद डोंगरी के नाम से जानते हैं। कच्चा-पक्का रास्ता और फिर सीढियों से उपर चढने के पश्चात फिर एक छोटी सी पहाडी और दिखाई पडती है जिसके शीर्ष तक पहुँचने की सुविधा के लिये स्थानीय प्रशासन ने लोहे की सीढियाँ लगा दी हैं। जैसे जैसे आप इस पहाडी पर चढने लगते हैं पत्थरों में स्थान स्थान पर शेर के पंजो जैसे निशान और महिष के खुर जैसे निशान क्रमिकता में दिखाई पडते हैं जैसे उनका आपस में यहाँ संघर्ष हुआ हो। इन एक जैसे निशानों का क्रम उँचाई के साथ लगातार बढता जाता है और शीर्ष पर यह ऐसा लगता है जैसे शेर और भैंसे के मध्य भयावह संघर्ष हुआ हो और उनके पैरों के निशान गुत्थमगुत्था दिखाई पडते हैं। शीर्ष पर ही वह स्थान चिन्हित किया गया है जहाँ मान्यता है कि महिषासुर यहाँ मारा गया था। इसी स्थान के बाईँ और जो चरणचिन्ह प्रतिलक्षित होते हैं उन्हें माँ दुर्गा का बताया जाता है। अपनी पुस्तक “देवलोक बडे डोंगर” में जानकारी देते हुए श्री जयराम पात्र लिखते हैं कि “पुरातन बस्तर में पूर्व में बसे सभी जाति के लोग हर शुभ कार्य का आरम्भ यहीं आदि शक्ति माँ की पूजा के पश्चात ही करते हैं। नवरात्रि पर्व के समय यहाँ पूरे अट्ठारह गढ बस्तर के देवी देवताओं के नाम से सेवा-पूजा की जाती है। यहाँ क्वाँर (आश्विन) नवरात्रि के समय सैंकडों वर्ष पूर्व से जोगी बिठाने की परम्परा रही है। यहाँ के नवरात्रि की निशाजात्रा का प्रशाद बस्तर दशहरा के बाहर रैनी के रथ में चढाया जाता है। यहाँ का प्रसाद चढाये बिना रथ कुम्हडाकोट से जगदलपुर नहीं लाया जाता (पृष्ठ -8)”।
महिषासुर को ले कर अपनी अपनी आस्थायें और विवाद हैं। बस्तर अंचल का बडे डोंगर क्षेत्र इतिहास, पुरातत्व और जनमान्यताओं के बीच आस्था और पर्यटन की दृष्टि से अपनी ठोस उपस्थिति दर्ज कराता है।
- राजीव रंजन प्रसाद
=======
[नवरात्रि पर विशेष आलेख श्रंखला, छठवीं कड़ी]
----------------------------------
महिषासुर के वध स्थल होने का दावा देश के अनेक स्थानों से किया जाता है, बस्तर का बडे डोंगर क्षेत्र भी उनमें से एक है। बस्तर की मान्यता पर विवेचना से पहले इसी कथन से जुडे कुछ प्रचलित स्थलों को जान लेते हैं। दक्षिण भारत का भव्य एतिहासिक शहर है मैसूर। मैसूर शब्द पर ध्यान दीजिये क्योंकि प्रचलित मान्यता है कि एक समय में मैसूर ही महिषासुर की राजधानी ‘महिसुर’ हुआ करती थी; तर्कपूर्ण लगता है कि महिसुर बदल कर मैसूर हो गया हो। मैसूर के निकट की चामुण्डा पर्वत की अवस्थिति है जहाँ यह माना जाता है कि महिषासुर का वध भी यहीं हुआ था। इसी तरह पूर्वी भारत अर्थात हिमांचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी शक्तिपीठ अवस्थित है। पुराणों के अनुसार देवी सती के नैन गिरने के कारण यह शक्तिपीठ स्थापित हुआ किंतु महिषासुर की कथा भी इसी स्थल से जुडी हुई मानी जाती है तथा उसका वध-स्थल भी यहीं पर माना जाता है। कहानियाँ और भी हैं; झारखण्ड के चतरा जिले का भी यह दावा है कि महिषासुर का वध वहीं हुआ। इसके तर्क में तमासीन जलप्रपात के निकट क्षेत्रों में प्रचलित कथा है कि नवरात्र के समय आज भी यहाँ तलवारों की खनक सुनाई देती है तथा यत्र-तत्र सिंदूर बिखरा हुआ देखा जा सकता है।
इन सभी कहानियों से अधिक प्रामाणिक मुझे वह संदर्भ लगता है जो बस्तर की मान्यताओं में अवस्थित है। बस्तर के जिस क्षेत्र का संदर्भ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह हमेशा से ही जंगली भैंसो के लिये विख्यात रहा है; पुनश्च भैंस अर्थात महिष। अपने विशाल स्वरूप और बलिष्ठ काठी के कारण बस्तर के महिष को कभी दैत्याकार लिखा गया तो कभी उसका विवरण भयावहतम शब्दों में प्राचीन पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया है। बस्तर के इन महिषों/जंगली भैंसों पर गल्सफर्ड की डायरी (1860) से लिया गया यह एक विवरण देखें – “इसकी एक सींग साढे अठहत्तर इंच लम्बी होती है। यदि हम मस्तक की खोपड़ी एक फुट चौड़ी माने तो यह सिर से पैर तक चौदह फुट ऊँचा होता है”। यदि इस कहानी का बस्तर से उद्गम माना जाये तो यहाँ के महिष पालतू नहीं थे तथा उनका शिकार किया जाता रहा है। वस्तुत: महिषासुर के वध से जुडी कहानी बस्तर के बड़े डोंगर क्षेत्र से मानी जाती है।
बडे डोंगर में मेरी अभिरुचि पुरातात्विक महत्व के अनेक कारणों से तो थी ही किंतु मैं उस महिषाद्वन्द्व पहाड़ को विशेष रूप से देखना चाहता था जिसे स्थानीय भैंसादोंद डोंगरी के नाम से जानते हैं। कच्चा-पक्का रास्ता और फिर सीढियों से उपर चढने के पश्चात फिर एक छोटी सी पहाडी और दिखाई पडती है जिसके शीर्ष तक पहुँचने की सुविधा के लिये स्थानीय प्रशासन ने लोहे की सीढियाँ लगा दी हैं। जैसे जैसे आप इस पहाडी पर चढने लगते हैं पत्थरों में स्थान स्थान पर शेर के पंजो जैसे निशान और महिष के खुर जैसे निशान क्रमिकता में दिखाई पडते हैं जैसे उनका आपस में यहाँ संघर्ष हुआ हो। इन एक जैसे निशानों का क्रम उँचाई के साथ लगातार बढता जाता है और शीर्ष पर यह ऐसा लगता है जैसे शेर और भैंसे के मध्य भयावह संघर्ष हुआ हो और उनके पैरों के निशान गुत्थमगुत्था दिखाई पडते हैं। शीर्ष पर ही वह स्थान चिन्हित किया गया है जहाँ मान्यता है कि महिषासुर यहाँ मारा गया था। इसी स्थान के बाईँ और जो चरणचिन्ह प्रतिलक्षित होते हैं उन्हें माँ दुर्गा का बताया जाता है। अपनी पुस्तक “देवलोक बडे डोंगर” में जानकारी देते हुए श्री जयराम पात्र लिखते हैं कि “पुरातन बस्तर में पूर्व में बसे सभी जाति के लोग हर शुभ कार्य का आरम्भ यहीं आदि शक्ति माँ की पूजा के पश्चात ही करते हैं। नवरात्रि पर्व के समय यहाँ पूरे अट्ठारह गढ बस्तर के देवी देवताओं के नाम से सेवा-पूजा की जाती है। यहाँ क्वाँर (आश्विन) नवरात्रि के समय सैंकडों वर्ष पूर्व से जोगी बिठाने की परम्परा रही है। यहाँ के नवरात्रि की निशाजात्रा का प्रशाद बस्तर दशहरा के बाहर रैनी के रथ में चढाया जाता है। यहाँ का प्रसाद चढाये बिना रथ कुम्हडाकोट से जगदलपुर नहीं लाया जाता (पृष्ठ -8)”।
महिषासुर को ले कर अपनी अपनी आस्थायें और विवाद हैं। बस्तर अंचल का बडे डोंगर क्षेत्र इतिहास, पुरातत्व और जनमान्यताओं के बीच आस्था और पर्यटन की दृष्टि से अपनी ठोस उपस्थिति दर्ज कराता है।
- राजीव रंजन प्रसाद
=======
आज जन्मदिवस : आचार्य रामचंद्र शुक्ल
आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तम्भ आचार्य शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1883 को अगोना, जिला -बस्ती (उप्र) में हुआ था।आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक विधि से विभाजित कर उसे 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (1928-29) के रूप में प्रस्तुत किया जो सदैव हिंदी विद्यार्थियों के लिए आधार पुस्तक रहेगी। शुक्ल जी एक ख्यात आलोचक, निबंधकार, कथाकार और संपादक थे।
'रस मीमांसा' और 'चिंतामणि' इनकी अन्य रचनाएँ हैं। द्विवेदी युग की परिमार्जित, परिनिष्ठित हिंदी को इन्होने आगे बढाया है। आज जो काल विभाजन और प्रवृत्तियाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जानते हैं, वे सभी आचार्य शुक्ल की ही देन है। शुक्ल जी ने अपने समय में अपना काम किया। उनके काम को आवश्यक नवीन शोधों आदि से हमे संशोधित, परिमार्जित और समृद्ध करना होगा।
आचार्य शुक्ल को उनके जन्म दिवस पर पुण्य स्मरण....
आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तम्भ आचार्य शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1883 को अगोना, जिला -बस्ती (उप्र) में हुआ था।आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक विधि से विभाजित कर उसे 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (1928-29) के रूप में प्रस्तुत किया जो सदैव हिंदी विद्यार्थियों के लिए आधार पुस्तक रहेगी। शुक्ल जी एक ख्यात आलोचक, निबंधकार, कथाकार और संपादक थे।
'रस मीमांसा' और 'चिंतामणि' इनकी अन्य रचनाएँ हैं। द्विवेदी युग की परिमार्जित, परिनिष्ठित हिंदी को इन्होने आगे बढाया है। आज जो काल विभाजन और प्रवृत्तियाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जानते हैं, वे सभी आचार्य शुक्ल की ही देन है। शुक्ल जी ने अपने समय में अपना काम किया। उनके काम को आवश्यक नवीन शोधों आदि से हमे संशोधित, परिमार्जित और समृद्ध करना होगा।
आचार्य शुक्ल को उनके जन्म दिवस पर पुण्य स्मरण....
जनता के राजा - प्रवीरचन्द्र भंजदेव .....!
प्रस्तुत चित्र 1962 के बस्तर के दशहरे का है जिसमे जनता के राजा , बस्तर के महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव जी महारानी वेदवती जी के साथ रथारूढ़ हुए थे.1961 मे महाराजा प्रवीरचन्द्र को अपदस्थ कर उनके छोटे भाई विजयचन्द्र को बस्तर का महाराजा घोषित कर दिया गया था. लाला जगदलपुरी जी अपनी पुस्तक बस्तर इतिहास एवँ संस्कृति मे कहते है कि शासन विजयचन्द्र भंजदेव द्वारा ही दशहरा मनाये जाने पर सहायता देने को राजी था. लेकिन विरोधी आदिवासियो के दिलो स्थापित प्रवीर के एकछत्र साम्राज्य को हिला ना सके. कभी दशहरे मे रथ पर सवार ना होने वाले प्रवीर "जनता के राजा" बनकर सपत्नीक रथ पर सवार हुए. लगभग 5 लाख आदिवासी बस्तर के कोने कोने से आकर दशहरे मे शामिल हुए. उनके लाखो समर्थक आदिवासियो ने दशहरे का खर्च उठाकर बस्तर के इतिहास में बेहद शानदार दशहरा मनाया. 1965 तक उनकी मृत्यु पर्यन्त तक सभी दशहरे बेहद शानदार ढंग से मनाये जाते रहे है.
प्रस्तुत चित्र 1962 के बस्तर के दशहरे का है जिसमे जनता के राजा , बस्तर के महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव जी महारानी वेदवती जी के साथ रथारूढ़ हुए थे.1961 मे महाराजा प्रवीरचन्द्र को अपदस्थ कर उनके छोटे भाई विजयचन्द्र को बस्तर का महाराजा घोषित कर दिया गया था. लाला जगदलपुरी जी अपनी पुस्तक बस्तर इतिहास एवँ संस्कृति मे कहते है कि शासन विजयचन्द्र भंजदेव द्वारा ही दशहरा मनाये जाने पर सहायता देने को राजी था. लेकिन विरोधी आदिवासियो के दिलो स्थापित प्रवीर के एकछत्र साम्राज्य को हिला ना सके. कभी दशहरे मे रथ पर सवार ना होने वाले प्रवीर "जनता के राजा" बनकर सपत्नीक रथ पर सवार हुए. लगभग 5 लाख आदिवासी बस्तर के कोने कोने से आकर दशहरे मे शामिल हुए. उनके लाखो समर्थक आदिवासियो ने दशहरे का खर्च उठाकर बस्तर के इतिहास में बेहद शानदार दशहरा मनाया. 1965 तक उनकी मृत्यु पर्यन्त तक सभी दशहरे बेहद शानदार ढंग से मनाये जाते रहे है.
आज जन्मदिवस : वीरांगना रानी दुर्गावती
सन 1524 की 5 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी थी जब बांदा (बुन्देलखण्ड) के चन्देल राजा कीर्तिसिंह के घर कालिंजर में कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया दुर्गा। दुर्गा में बचपन से ही बुद्धि, साहस, अनुशासन और सैन्य कुशलताएं विकसित हो गयी थीं। युवावस्था में दुर्गा से विवाह के लिए गढ़मंडला (गोंडवाना राज्य) के गोंड राजा संग्राम सिंह मडावी ने अपने पुत्र दलपत शाह के लिए दुर्गा का हाथ मांगा पर कीर्तिसिंह ने इनकार किया और युद्ध की स्थिति आ गयी जिसमें महोबा की सेना को गोंडवाना की सेना ने पराजित कर दिया। इस युद्ध का परिणाम दलपतशाह और दुर्गा के विवाह के रूप में संम्पन्न हुआ।
दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी थी। उसका राज्य वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास का था। दुर्गावती के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीर नारायण था। चार वर्ष बाद दलपतशाह की मृत्यु हो गयी। ऐसे में दुर्गावती ने धैर्य और हौसले से गोंडवाना राज्य को एक बुद्धिमान मंत्री आधारसिंह के सहयोग से संचालित किया। उसने राज्य का विस्तार किया और उसे मजबूती प्रदान की। दुर्गावती को मालवा के शासक बाजबहादुर ने कई बार हमले करके परेशान किया और हर बार उसने उसे माकूल जवाब दिया। 1563-64 में अकबर का सिपहसालार आसफ खां जो इलाहाबाद का सूबेदार था, गोंडवाना पर हमला किया जिसे दुर्गावती ने विफल कर दिया। ऐसे और प्रयास हुए। जून 1564 के तीसरे हमले में आसफ खां ने बड़ा हमला बोला। दुर्गावती ने सैनिक वेश में अपनी सेना का संचालन किया। उसने नरई नाले के पास अपना मोर्चा लगाया। युद्ध मे उसके युवा पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो गयी और रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस का परिचय देते युद्ध किया और अंततः बुरी तरह घायल हुई। 24 जून 1564 को जीवित पकड़े जाने और प्रताड़ित होने की संभावना को देखते हुए उसने खुद को कटार मारकर खत्म कर लिया!
रानी दुर्गावती एक योग्य शासिका थी। उसने 16 वर्षों तक गोंडवाना की कुशलतापूर्वक कमान संभाली। जबलपुर में उसने अपनी दासी की स्मृति में चेरीताल, मंत्री आधारसिंह के नाम पर आधारताल और स्वयं के नाम पर रानीताल का निर्माण करवाया था। दुर्गावती की समाधि बरेला में है। जबलपुर के पहले विवि का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर ही है। नवरात्रि में जन्मी दुर्गा ने अपने नाम को सिद्ध किया। भारतीय समाज को चाहिए कि वह सिर्फ दुर्गा पूजन तक स्वयं को सीमित न रखे बल्कि बेटियों को शिक्षा और बल प्रदान करे ताकि एक बेहतर समाज की स्थापना हो सके।
जन्मदिन पर वीरांगना रानी दुर्गावती को सलाम !
सन 1524 की 5 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी थी जब बांदा (बुन्देलखण्ड) के चन्देल राजा कीर्तिसिंह के घर कालिंजर में कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया दुर्गा। दुर्गा में बचपन से ही बुद्धि, साहस, अनुशासन और सैन्य कुशलताएं विकसित हो गयी थीं। युवावस्था में दुर्गा से विवाह के लिए गढ़मंडला (गोंडवाना राज्य) के गोंड राजा संग्राम सिंह मडावी ने अपने पुत्र दलपत शाह के लिए दुर्गा का हाथ मांगा पर कीर्तिसिंह ने इनकार किया और युद्ध की स्थिति आ गयी जिसमें महोबा की सेना को गोंडवाना की सेना ने पराजित कर दिया। इस युद्ध का परिणाम दलपतशाह और दुर्गा के विवाह के रूप में संम्पन्न हुआ।
दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी थी। उसका राज्य वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास का था। दुर्गावती के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीर नारायण था। चार वर्ष बाद दलपतशाह की मृत्यु हो गयी। ऐसे में दुर्गावती ने धैर्य और हौसले से गोंडवाना राज्य को एक बुद्धिमान मंत्री आधारसिंह के सहयोग से संचालित किया। उसने राज्य का विस्तार किया और उसे मजबूती प्रदान की। दुर्गावती को मालवा के शासक बाजबहादुर ने कई बार हमले करके परेशान किया और हर बार उसने उसे माकूल जवाब दिया। 1563-64 में अकबर का सिपहसालार आसफ खां जो इलाहाबाद का सूबेदार था, गोंडवाना पर हमला किया जिसे दुर्गावती ने विफल कर दिया। ऐसे और प्रयास हुए। जून 1564 के तीसरे हमले में आसफ खां ने बड़ा हमला बोला। दुर्गावती ने सैनिक वेश में अपनी सेना का संचालन किया। उसने नरई नाले के पास अपना मोर्चा लगाया। युद्ध मे उसके युवा पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो गयी और रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस का परिचय देते युद्ध किया और अंततः बुरी तरह घायल हुई। 24 जून 1564 को जीवित पकड़े जाने और प्रताड़ित होने की संभावना को देखते हुए उसने खुद को कटार मारकर खत्म कर लिया!
रानी दुर्गावती एक योग्य शासिका थी। उसने 16 वर्षों तक गोंडवाना की कुशलतापूर्वक कमान संभाली। जबलपुर में उसने अपनी दासी की स्मृति में चेरीताल, मंत्री आधारसिंह के नाम पर आधारताल और स्वयं के नाम पर रानीताल का निर्माण करवाया था। दुर्गावती की समाधि बरेला में है। जबलपुर के पहले विवि का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर ही है। नवरात्रि में जन्मी दुर्गा ने अपने नाम को सिद्ध किया। भारतीय समाज को चाहिए कि वह सिर्फ दुर्गा पूजन तक स्वयं को सीमित न रखे बल्कि बेटियों को शिक्षा और बल प्रदान करे ताकि एक बेहतर समाज की स्थापना हो सके।
जन्मदिन पर वीरांगना रानी दुर्गावती को सलाम !
स्वामी आत्मानंद जी।
🍁🍁🍁🍁🍁🍁
आज मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र क्षेत्र में "रामकृष्ण-विवेकानंद- भावधारा" के अग्रणी प्रचारक परमपूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज का जन्म-दिवस है।
महाराज का जन्म 06 अक्टूबर 1929 को रायपुर जिले के बरबंदा ग्राम में हुआ था। पिता श्री धनीराम वर्मा ,माता श्रीमती भाग्यवती देवी,के इस ज्येष्ठ सुपुत्र के साथ-साथ अन्य संताने,स्वामी निखिलात्मानंद,स्वामी त्यागात्मानंद, डॉ.नरेंद्रदेव वर्मा ,प्रसिद्ध भाषाविद्,डॉ.ओमप्रकाश वर्मा
पूर्व अध्यक्ष,वि.वि.नियामक आयोग,छ.ग., डॉ.लक्ष्मी धुरंधर,प्राध्यापिका अर्थशास्त्र,ने भी अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की।
पूज्य महाराज जी की स्कूली शिक्षा,सेंट पॅाल्स स्कूल रायपुर और महाविद्यालय शिक्षा,(एमएससी गणित) नागपुर विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने आईएएस की परीक्षा दी और प्रथम 10 स्थानों में चयनित हुए ,परंतु मौखिक परीक्षा न देकर श्रीरामकृष्ण मिशन में प्रवेश ले लिया।
महाराज की ब्रह्मचर्य-दीक्षा, सन् 1957 में श्रीरामकृष्ण संघ के तत्कालीन परमाध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी शंकरानंद जी महाराज द्वारा हुई और उन्हें ब्रह्मचारी 'तेजचैतन्य 'का नाम मिला।
महाराज के मन में सदैव यह बात रहती थी कि अपने बाल्यकाल में स्वामी विवेकानंद जी ने दो वर्ष की अवधि रायपुर में बितायी हैं। इस स्मृति को एक स्वरूप देकर स्थायी करने का विचार आने पर उन्होंने 'विवेकानंद आश्रम रायपुर' की नींव डाली। महाराज के अथक
प्रयास और छत्तीसगढ़ की जनता के सहयोग से इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। कालांतर में "रामकृष्ण
मिशन "ने इस संस्था को अधिग्रहित कर लिया।
महाराज की समस्त चेतना,"आत्मनो मोक्षार्थम,जगद् हिताय च,तथा"शिव-भाव से जीव-सेवा" से अनुप्राणित
थी। उनके कठिन प्रयासों से,रायपुर में श्रीरामकृष्णदेव
के मंदिर का निर्माण हो रहा था तभी छत्तीसगढ़ को 'दुर्भिक्ष' का सामना करना पड़ा। उन्होंने मंदिर निर्माण
का कार्य रोक दिया और संचित धन का उपयोग राहत-कार्यों के संचालन में कर दिया। हम सब,तब विवेकानंद-विद्यार्थी-भवन के छात्र थे और इन घटनाओं के स्वयं साक्षी हैं।
वनवासियों की समग्र शिक्षा और उत्थान के प्रति उनका इतना तीव्र आग्रह था कि उन्होंने 'नारायणपुर',बस्तर जिले में ,एक"वनवासी-सेवा-प्रकल्प" का निर्माण किया, जहां बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय जन को ,
कृषि-संवर्धन की जानकारियां दी जाती हैं ।अब यह संस्थान और भी कई क्षेत्रों में उन्नति कर विशाल स्वरूप धारण कर चुका है।
पूज्य महाराज से अनुप्रेरित होकर अनेक विशिष्ट-जनों
ने स्वयं को रामकृष्ण मिशन में सम्मिलित किया। जिनमें
परमपूज्य स्वामी सत्यरूपानंद,स्वामी निखिलात्मानंद, स्वामी ब्रह्मेशानंद,स्वामी श्रीकरानंद,स्वामी त्यागात्मानंद, स्वामी निखिलेश्वरानंद, स्वामी अव्ययानंद, स्वामी जयदानंद, स्वामी चिरंतनानंद,आदि वे हैं,जिन्हें मैं स्वयं जानता हूं। ऐसे और भी कई साधु/ब्रह्मचारी हुए होंगे, जिन्होंने उनसे "रामकृष्ण-विवेकानंद-भाव-धारा" में सम्मिलित होने की प्रेरणा पायी होगी।
महाराज ने 27 अगस्त 1989 को अपने स्वरूप को समेट लिया, और श्रीरामकृष्णधाम को प्रस्थान कर
गये।
म.प्र.एवं छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए अपने कई जनकल्याणकारी योजनाओं को ,
उनके नाम पर 'अर्पित 'किया है।
शुभ जन्मदिवस, महाराज!
जय मां दुर्गा,
🍁🍁🍁🍁🍁🍁
आज मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र क्षेत्र में "रामकृष्ण-विवेकानंद- भावधारा" के अग्रणी प्रचारक परमपूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज का जन्म-दिवस है।
महाराज का जन्म 06 अक्टूबर 1929 को रायपुर जिले के बरबंदा ग्राम में हुआ था। पिता श्री धनीराम वर्मा ,माता श्रीमती भाग्यवती देवी,के इस ज्येष्ठ सुपुत्र के साथ-साथ अन्य संताने,स्वामी निखिलात्मानंद,स्वामी त्यागात्मानंद, डॉ.नरेंद्रदेव वर्मा ,प्रसिद्ध भाषाविद्,डॉ.ओमप्रकाश वर्मा
पूर्व अध्यक्ष,वि.वि.नियामक आयोग,छ.ग., डॉ.लक्ष्मी धुरंधर,प्राध्यापिका अर्थशास्त्र,ने भी अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की।
पूज्य महाराज जी की स्कूली शिक्षा,सेंट पॅाल्स स्कूल रायपुर और महाविद्यालय शिक्षा,(एमएससी गणित) नागपुर विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने आईएएस की परीक्षा दी और प्रथम 10 स्थानों में चयनित हुए ,परंतु मौखिक परीक्षा न देकर श्रीरामकृष्ण मिशन में प्रवेश ले लिया।
महाराज की ब्रह्मचर्य-दीक्षा, सन् 1957 में श्रीरामकृष्ण संघ के तत्कालीन परमाध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी शंकरानंद जी महाराज द्वारा हुई और उन्हें ब्रह्मचारी 'तेजचैतन्य 'का नाम मिला।
महाराज के मन में सदैव यह बात रहती थी कि अपने बाल्यकाल में स्वामी विवेकानंद जी ने दो वर्ष की अवधि रायपुर में बितायी हैं। इस स्मृति को एक स्वरूप देकर स्थायी करने का विचार आने पर उन्होंने 'विवेकानंद आश्रम रायपुर' की नींव डाली। महाराज के अथक
प्रयास और छत्तीसगढ़ की जनता के सहयोग से इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। कालांतर में "रामकृष्ण
मिशन "ने इस संस्था को अधिग्रहित कर लिया।
महाराज की समस्त चेतना,"आत्मनो मोक्षार्थम,जगद् हिताय च,तथा"शिव-भाव से जीव-सेवा" से अनुप्राणित
थी। उनके कठिन प्रयासों से,रायपुर में श्रीरामकृष्णदेव
के मंदिर का निर्माण हो रहा था तभी छत्तीसगढ़ को 'दुर्भिक्ष' का सामना करना पड़ा। उन्होंने मंदिर निर्माण
का कार्य रोक दिया और संचित धन का उपयोग राहत-कार्यों के संचालन में कर दिया। हम सब,तब विवेकानंद-विद्यार्थी-भवन के छात्र थे और इन घटनाओं के स्वयं साक्षी हैं।
वनवासियों की समग्र शिक्षा और उत्थान के प्रति उनका इतना तीव्र आग्रह था कि उन्होंने 'नारायणपुर',बस्तर जिले में ,एक"वनवासी-सेवा-प्रकल्प" का निर्माण किया, जहां बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय जन को ,
कृषि-संवर्धन की जानकारियां दी जाती हैं ।अब यह संस्थान और भी कई क्षेत्रों में उन्नति कर विशाल स्वरूप धारण कर चुका है।
पूज्य महाराज से अनुप्रेरित होकर अनेक विशिष्ट-जनों
ने स्वयं को रामकृष्ण मिशन में सम्मिलित किया। जिनमें
परमपूज्य स्वामी सत्यरूपानंद,स्वामी निखिलात्मानंद, स्वामी ब्रह्मेशानंद,स्वामी श्रीकरानंद,स्वामी त्यागात्मानंद, स्वामी निखिलेश्वरानंद, स्वामी अव्ययानंद, स्वामी जयदानंद, स्वामी चिरंतनानंद,आदि वे हैं,जिन्हें मैं स्वयं जानता हूं। ऐसे और भी कई साधु/ब्रह्मचारी हुए होंगे, जिन्होंने उनसे "रामकृष्ण-विवेकानंद-भाव-धारा" में सम्मिलित होने की प्रेरणा पायी होगी।
महाराज ने 27 अगस्त 1989 को अपने स्वरूप को समेट लिया, और श्रीरामकृष्णधाम को प्रस्थान कर
गये।
म.प्र.एवं छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए अपने कई जनकल्याणकारी योजनाओं को ,
उनके नाम पर 'अर्पित 'किया है।
शुभ जन्मदिवस, महाराज!
जय मां दुर्गा,
बस्तर दशहरा में बेल पूजा की रस्म......!
शहर से लगे ग्राम सरगीपाल में बेल पूजा होती है। यहां राजपरिवार और अन्य श्रद्धालु बेल पेड़ पर पूजा-अनुष्ठान के बाद युग्म बेल फल लेकर दंतेश्वरी मंदिर आते है। ग्रामीण गाजे-बाजे के साथ पूजा के बाद विवाह की भांति एक-दूसरे को तेल-हल्दी लगाकर लोगों का स्वागत व विदाई करते है।
बस्तर दशहरा में फूल रथ की पांचवीं परिक्रमा के बाद सोमवार की देर रात दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी व मांझी-मुखिया सरगीपाल जाते है। जहां बरसों पुराने बेल फल के वृक्ष के तले देवी का आव्हान करते युग्म (जोड़ा) बेल फल को कपड़े से बांधते है। पूजा-अनुष्ठान के बाद दो बकरों की बलि दी जाएगी और युग्म फल को तोड़ दंतेश्वरी मंदिर लाकर प्रतिस्थापित किया जाएगा।
परंपरानुसार बरसों से दशहरा के दौरान अश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी को बेल पूजा की जाती है। इस रस्म को ग्रामीण पुत्री विवाह की तरह मानते हैं। पूजा के बाद वे एक-दूसरे पर हल्दी-पानी का छींटा मारते हैं।
ग्रामीण मान्यता के अनुसार बेल पेड़ व फल को ग्रामीण माता दुर्गा का दूसरा रूप मानते हैं, इसलिए दशहरा के मौके पर फूल रथ की पांचवी परिक्रमा पूर्ण होने के बाद बेल न्यौता व बेल पूजा की जाती है।
फोटो सौजन्य अजय सिंह जी
शहर से लगे ग्राम सरगीपाल में बेल पूजा होती है। यहां राजपरिवार और अन्य श्रद्धालु बेल पेड़ पर पूजा-अनुष्ठान के बाद युग्म बेल फल लेकर दंतेश्वरी मंदिर आते है। ग्रामीण गाजे-बाजे के साथ पूजा के बाद विवाह की भांति एक-दूसरे को तेल-हल्दी लगाकर लोगों का स्वागत व विदाई करते है।
बस्तर दशहरा में फूल रथ की पांचवीं परिक्रमा के बाद सोमवार की देर रात दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी व मांझी-मुखिया सरगीपाल जाते है। जहां बरसों पुराने बेल फल के वृक्ष के तले देवी का आव्हान करते युग्म (जोड़ा) बेल फल को कपड़े से बांधते है। पूजा-अनुष्ठान के बाद दो बकरों की बलि दी जाएगी और युग्म फल को तोड़ दंतेश्वरी मंदिर लाकर प्रतिस्थापित किया जाएगा।
परंपरानुसार बरसों से दशहरा के दौरान अश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी को बेल पूजा की जाती है। इस रस्म को ग्रामीण पुत्री विवाह की तरह मानते हैं। पूजा के बाद वे एक-दूसरे पर हल्दी-पानी का छींटा मारते हैं।
ग्रामीण मान्यता के अनुसार बेल पेड़ व फल को ग्रामीण माता दुर्गा का दूसरा रूप मानते हैं, इसलिए दशहरा के मौके पर फूल रथ की पांचवी परिक्रमा पूर्ण होने के बाद बेल न्यौता व बेल पूजा की जाती है।
फोटो सौजन्य अजय सिंह जी
माई जी को बस्तर दशहरा का निमंत्रण.....!
भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य के लिये सबसे पहले देवी देवताओं को याद किया जाता है। उनकी पूजा अर्चना के बाद ही मांगलिक कार्य संपन्न किये जाते है। कुछ रस्मों रिवाजों एवं कार्यक्रमों देवी देवताओं की उपस्थिति बेहद ही अनिवार्य होती है।
बस्तर दशहरा में भी देवी दंतेश्वरी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। बस्तर में देवी दंतेश्वरी के बिना दशहरा पर्व संभव ही नहीं है। देवी दंतेश्वरी दसवी सदी पूर्व से वर्तमान काल तक बस्तर की आराध्या देवी है। पूर्व में नागवंशी राजाओं एवं परवर्ती काकतीय चालुक्य राजाओं ने देवी को अपनी ईष्ट देवी मानकर आराधना की।
नागयुगीन माणिक्यदेवी ही काकतीय राज में दंतेश्वरी के नाम से जानी गई। नागराजाओं ने माणिक्यदेवी के सम्मान में हर तरह के आयोजन किये उसी प्रकार काकतीय चालुक्य राजाओं में अन्नमदेव और बाद पुरूषोत्तम देव ने देवी की उपस्थिति में दशहरे और फाल्गुन मेले का प्रारंभ किया।
देवी दंतेश्वरी को सुमिरन किये बिना बस्तर में आज भी कोई शुुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। दशहरा में देवी दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर जाती है। देवी के छत्र को राजा या पुजारी अपने हाथों में लेकर रथारूढ़ होते है। देवी के छत्र को रथ पर विराजित की रथ परिक्रमा की परंपरा निर्वहन की जाती है।
आश्विन शुक्ल पंचमी को राज परिवार के सदस्य, मांझी चालकियों का दल जगदलपुर से दंतेवाड़ा में माई जी के मंदिर में दशहरा निमंत्रण देने के लिये आते है। निमंत्रण के लिये विनय पत्रिका राजगुरू द्वारा संस्कृत में लिखी जाती है। विनय पत्रिका , अक्षत सुपारी सहित बस्तर महाराजा के द्वारा देवी दंतेश्वरी के चरणो में अर्पित की जाती है।
देवी से दशहरा में सम्मिलित होने की गुहार लगाई जाती है। न्यौते को स्वीकार करने के बाद देवी के प्रतीक मावली माता की प्रतिमा जो नये कपड़े में हल्दी का लेप लगाकर बनायी जाती है। मावली देवी को पूजा अर्चना कर डोली में विराजित किया जाता है।
देवी दंतेश्वरी का अन्य नाम मावली देवी भी है। डोली को गर्भगृह से बाहर मंदिर के सभाकक्ष में रखा जाता है। पंचमी से अष्टमी तक देवी की डोली सभाकक्ष में स्थापित रहती है। अष्टमी को देवी दंतेश्वरी की डोली पुजारी एवं सेवादार के साथ जगदलपुर रवाना होती है। पहले रियासतकाल में राजा भैरमदेव के समय चांदी की डोली होती थी। महारानी प्रफुल्लकुमारी के समय देवी की डोली रक्त चंदन की लकड़ी से बनाई गई थी.
दंतेवाड़ा से देवी की डोली की रवानगी....!
बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी अष्टमी को ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने जगदलपुर रवाना होती है। मांईजी के छत्र व डोली को मंदिर परिसर में सलामी दी जाती है। माईंजी की डोली के साथ पुजारी सेवादार समरथ मांझी व चालकी के साथ 12 परगना के लोग शामिल होतेे है। डोली और छत्र मंदिर से आतिशबाजी के साथ निकलते है।
तत्पश्चात डंकनी नदी के पास बनाए गए पूजा स्थल में श्रद्धालु पूजा.अर्चना कर मांईजी को विदा करते। आंवराभाटा से मांईजी की डोली व छत्र फूलों से सजे वाहन में जगदलपुर रवाना होती है।
रियासत काल में माईजी को जगदलपुर पहुंचने में तीन चार दिन लग जाते थे। सेवादार डोली को कंधो पर उठाकर पैदल जगदलपुर पहुंचते थे। अब वाहन के कारण नवमीं की सुबह को डोली जगदलपुर पहुंच जाती है।
दंतेवाड़ा से जगदलपुर तक आवराभाठा हारम गीदम बास्तानार किलेपाल कोडेनार डिलमिली तोकापाल पंडरीपानी मे देवी का स्वागत सत्कार किया जाता है। हजारों श्रद्धालु देवी के स्वागत एवं पूजा अर्चना के लिये पलके बिछाये खड़े रहते है। रात्रि को जगदलपुर में जिया डेरा विश्राम करती है। सुबह देवी की स्वागत एवं पूजा अर्चना की जाती है।
ओम
भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य के लिये सबसे पहले देवी देवताओं को याद किया जाता है। उनकी पूजा अर्चना के बाद ही मांगलिक कार्य संपन्न किये जाते है। कुछ रस्मों रिवाजों एवं कार्यक्रमों देवी देवताओं की उपस्थिति बेहद ही अनिवार्य होती है।
बस्तर दशहरा में भी देवी दंतेश्वरी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। बस्तर में देवी दंतेश्वरी के बिना दशहरा पर्व संभव ही नहीं है। देवी दंतेश्वरी दसवी सदी पूर्व से वर्तमान काल तक बस्तर की आराध्या देवी है। पूर्व में नागवंशी राजाओं एवं परवर्ती काकतीय चालुक्य राजाओं ने देवी को अपनी ईष्ट देवी मानकर आराधना की।
नागयुगीन माणिक्यदेवी ही काकतीय राज में दंतेश्वरी के नाम से जानी गई। नागराजाओं ने माणिक्यदेवी के सम्मान में हर तरह के आयोजन किये उसी प्रकार काकतीय चालुक्य राजाओं में अन्नमदेव और बाद पुरूषोत्तम देव ने देवी की उपस्थिति में दशहरे और फाल्गुन मेले का प्रारंभ किया।
देवी दंतेश्वरी को सुमिरन किये बिना बस्तर में आज भी कोई शुुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। दशहरा में देवी दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर जाती है। देवी के छत्र को राजा या पुजारी अपने हाथों में लेकर रथारूढ़ होते है। देवी के छत्र को रथ पर विराजित की रथ परिक्रमा की परंपरा निर्वहन की जाती है।
आश्विन शुक्ल पंचमी को राज परिवार के सदस्य, मांझी चालकियों का दल जगदलपुर से दंतेवाड़ा में माई जी के मंदिर में दशहरा निमंत्रण देने के लिये आते है। निमंत्रण के लिये विनय पत्रिका राजगुरू द्वारा संस्कृत में लिखी जाती है। विनय पत्रिका , अक्षत सुपारी सहित बस्तर महाराजा के द्वारा देवी दंतेश्वरी के चरणो में अर्पित की जाती है।
देवी से दशहरा में सम्मिलित होने की गुहार लगाई जाती है। न्यौते को स्वीकार करने के बाद देवी के प्रतीक मावली माता की प्रतिमा जो नये कपड़े में हल्दी का लेप लगाकर बनायी जाती है। मावली देवी को पूजा अर्चना कर डोली में विराजित किया जाता है।
देवी दंतेश्वरी का अन्य नाम मावली देवी भी है। डोली को गर्भगृह से बाहर मंदिर के सभाकक्ष में रखा जाता है। पंचमी से अष्टमी तक देवी की डोली सभाकक्ष में स्थापित रहती है। अष्टमी को देवी दंतेश्वरी की डोली पुजारी एवं सेवादार के साथ जगदलपुर रवाना होती है। पहले रियासतकाल में राजा भैरमदेव के समय चांदी की डोली होती थी। महारानी प्रफुल्लकुमारी के समय देवी की डोली रक्त चंदन की लकड़ी से बनाई गई थी.
दंतेवाड़ा से देवी की डोली की रवानगी....!
बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी अष्टमी को ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने जगदलपुर रवाना होती है। मांईजी के छत्र व डोली को मंदिर परिसर में सलामी दी जाती है। माईंजी की डोली के साथ पुजारी सेवादार समरथ मांझी व चालकी के साथ 12 परगना के लोग शामिल होतेे है। डोली और छत्र मंदिर से आतिशबाजी के साथ निकलते है।
तत्पश्चात डंकनी नदी के पास बनाए गए पूजा स्थल में श्रद्धालु पूजा.अर्चना कर मांईजी को विदा करते। आंवराभाटा से मांईजी की डोली व छत्र फूलों से सजे वाहन में जगदलपुर रवाना होती है।
रियासत काल में माईजी को जगदलपुर पहुंचने में तीन चार दिन लग जाते थे। सेवादार डोली को कंधो पर उठाकर पैदल जगदलपुर पहुंचते थे। अब वाहन के कारण नवमीं की सुबह को डोली जगदलपुर पहुंच जाती है।
दंतेवाड़ा से जगदलपुर तक आवराभाठा हारम गीदम बास्तानार किलेपाल कोडेनार डिलमिली तोकापाल पंडरीपानी मे देवी का स्वागत सत्कार किया जाता है। हजारों श्रद्धालु देवी के स्वागत एवं पूजा अर्चना के लिये पलके बिछाये खड़े रहते है। रात्रि को जगदलपुर में जिया डेरा विश्राम करती है। सुबह देवी की स्वागत एवं पूजा अर्चना की जाती है।
ओम